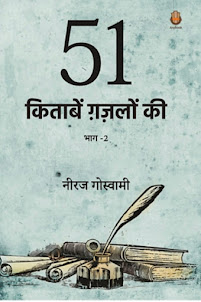अज़ीब है ये सतरंगी शोहरत की चिड़िया। मैंने देखा है कि अक्सर इसे जिस नाम की मुंडेर पर बैठ कर चहचहाना होता है उसे छोड़ ऐसी मुंडेर पर बैठ कर गीत गाती है जो इस लायक भी नहीं होती कि उस पर कव्वे बैठ कर काँव काँव करें। शोहरत की चिड़िया को अपने नाम की मुंडेर पर बिठाने के लिए लोग क्या नहीं करते। कुछ ने इस काम के लिए गुर्गे पाले हुए हैं जो किसी न किसी तरह जोड़ तोड़ कर इस चिड़िया को उनके नाम की मुंडेर पर बिठा कर फिर उसे वहां से उड़ने ही नहीं देते। अधिकतर ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि उनके नाम की मुंडेर इस लायक नहीं है कि उस पर ये चिड़िया बैठे तो वो इस फ़िराक में रहते हैं कि ये चिड़िया भले ही उनके नाम की मुंडेर से दूर रहे लेकिन किसी परिचित की मुंडेर पर भी न बैठ पाए।
अगर आप किसी के नाम की मुंडेर पर शोहरत की सतरंगी चिड़िया चहचहाती देखें तो आँख मीच कर ये न मान लें कि उस नाम की मुंडेर इस लायक है कि उस पर बैठ ये चिड़िया चहचहाये और अगर किसी नाम की मुंडेर पर इस चिड़िया को चहचहाते न देखें तो ये भी न समझें कि वो मुंडेर इस लायक नहीं है। कहने का मतलब ये कि शोहरत हमेशा हुनरमंद के हिस्से में ही आये ये जरूरी नहीं है। हमारे आज के शायर ऐसे ही हैं जिनके नाम की मुंडेर पर शोहरत की चिड़िया को चहचहाने नहीं दिया गया। शोहरत की चिड़िया इनके नाम की मुंडेर पर नहीं आयी ऐसा नहीं है लेकिन उसे टिक कर बैठने नहीं दिया गया। इस वज़ह से इनके समकालीनों, जिनमें ज़फर इक़बाल ,जॉन एलिया ,अहमद फ़राज़ , नासिर काज़मी ,बशीर बद्र और निदा फ़ाज़ली आदि हैं, को जितनी शोहरत हासिल हुई उतनी तो क्या उसका दस प्रतिशत भी इनके हिस्से नहीं आयी।
वह टूटते हुए रिश्तों का हुस्ने-आख़िर था
कि चुप सी लग गई दोनों को बात करते हुए
*
मुझको इस दिलचस्प सफ़र की राह नहीं खोटी करनी
मैं उजलत में नहीं हूं यारों अपना रास्ता देखो तुम
आंँख से आंँख न जोड़ कर देखो सूए-उफ़ुक़ ऐ हमसफ़रो
लाखों रंग नज़र आएंगे तन्हा-तन्हा देखो तुम
अब तो तुम्हारे भी अंदर की बोल रही है मायूसी
मुझको समझाने बैठे हो अपना लहजा देखो तुम
*
जो मेरे वास्ते कल ज़हर बनके निकलेगा
तेरे लबों पे संँभलता हुआ सा कुछ तो है
यह मैं नहीं न सही अपने सर्द बिस्तर पर
ये करवटें बदलता हुआ सा कुछ तो है
*
किसी की लौटने की जब सदा सुनी तो खुला
कि मेरे साथ कोई और भी सफ़र में था
कोई भी घर में समझता न था मेरे दुख सुख
इक अजनबी की तरह मैं खुद अपने घर में था
*
ऐ सफ़े-अब्रे-रवाँ तेरे बाद
एक घना साया शजर से निकला
सफ़े-अब्रे-रवाँ : गतीशील बादल
*
कहीं से आ गया एक अब्र दरमियांँ वरना
मेरे बदन में ये सूरज उतरने वाला था
जब भी कोई इंसान लीक से हटकर काम करता है तो लीक पर चलने वाले उस पर दो तरह से प्रतिक्रिया देते हैं पहली या तो उसे सिरे से नकार देते हैं क्यूंकि अपने बनाये रास्ते पर चलने वाला उन्हें इस ग्रह का बंदा नहीं लगता और या उसकी पूजा करने लगते हैं। अफ़सोस हमारे आज के शायर के साथ लीक पर चलने वालों ने पहले वाला सलूक किया। कारण - इस शायर ने ऐसी भाषा को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया जो इससे पहले किसी शायर ने नहीं अपनायी थी। लीक पर चलने वाले उसे ठीक से समझ ही नहीं पाए। लोकप्रिय बनाने के जो आवश्यक तत्व शायरी में डाले जाते हैं वो इस शायर की शायरी में सिरे से ग़ायब थे। न गुलो बुलबुल थी न विसाल ओ हिज़्र की बातें थीं न महबूब के हुस्न की चर्चा थी न छलकती शराब के पैमाने थे। ज़िन्दगी को बिना किसी मिलावट के पेश करने वाली इस शायर की शायरी खालिस और सच्ची थी। शायद यही कारण है कि इनका नाम जितने लोगों को जानना चाहिए था उतने नहीं जान पाए। हिंदी पढ़ने लिखने वालों ने तो शायद ही इनका नाम कभी सुना हो क्यूंकि न तो इनकी कोई किताब हिंदी में उपलब्ध है और न ही ये बहुत अधिक हिंदी अखबारों या पत्रिकाओं में छपे हैं। इंटरनेट पर भी इनके बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती। इस मोतबर शायर का नाम है राजेंद्र मनचंदा बानी।
क़ौमी उर्दू काउंसिल ने सं 2017 में कुलियात-ऐ-बानी हिंदी में शाया की है । 383 पेज की इस किताब में बानी जी की चुनिंदा ग़ज़लें और नज़्में संकलित की गयी हैं। इस किताब को आप जनाब शादाब शेख़ को 9329669919 पर फोन या वाट्सऐप कर मंगवा सकते हैं। जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी के जनाब गोविन्द प्रसाद जी ने इसका हिंदी लिप्यांतरण किया है।
लगा जो पीठ में आकर वह तीर था किसका
मैं दुश्मनों की सफ़ों में न मरने वाला था
सफ़ों: पंक्तियाँ
*
अनबन गहरी हो जाएगी यूंँ ही समय गुजरने पर
उसको मनाना चाहोगे जब बस न चलेगा देखो तुम
सच कहते हो इन राहों पर चैन से आते जाते हो
अब थोड़ा इस क़ैद से निकलो कुछ अनदेखा देखो तुम
*
कैसे-कैसे मक़ाम आए हैं
मैं हुआ हूँ कहांँ-कहांँ ख़ाली
*
वो चाहता ये होगा कि मैं ही उसे बुलाऊँ
मेरी तरह वो फिरता है तन्हा यहीं कहीं
*
भरे शहर में इक बयाबाँ भी था
इशारा था अपने ही घर की तरफ़
*
कौन दे आवाज खाली रात के अंधे कुँएंँ में
कौन उतरे ख़्वाब से महरूम बिस्तर में अकेला
महरूम: वंचित
*
आ मिलाऊँ तुझे इक शख्स़ से आईने में
जिसका सर शाह का है हाथ सवाली का है
*
मैं उसके पांव की जंजीर देखता था बहुत
कुछ आशना न था आपनी ही मुश्किलों से मैं
मैं क्यों बुराई सुनूँ दोस्तों की ऐ बानी
अलग नहीं इन्हीं खोटे-खरे दिलों से मैं
सत्तर के दशक में, पाकिस्तान से हिजरत करने वाले करतार सिंह दुग्गल, फ़िक्र तौंसवीं, अमृता प्रीतम, गोपाल मित्तल, जोगिन्दर पॉल, प्रकाश पंडित, कुमार पाशी, नन्द किशोर, वेदपाल अश्क, हीरानंद सोज़, दिलीप सिंह और देवेंद्र सत्यार्थी जैसे लोगों ने उर्दू का एक ज़िंदा और सेक्युलर माहौल तरतीब किया था आज उसका तसव्वुर करना भी मुहाल है। ये सभी अलग सोच के लोग थे और आपस में खीर और शकर की तरह एक दूसरे में घुले मिले नहीं थे। ये लोग अलग ग्रुपों और टोलियों में बटे हुए थे इनमें एका भी था और विचारों का मतभेद भी, दोस्ती भी थी तो दुश्मनी भी एक दूसरे को कभी गालियाँ बकते तो थोड़ी ही देर में एक ही बीड़ी या सिगरेट के बारी बारी से कश खींचने लगते। ये लोग रिसाले निकालते जो कुछ वक़्त बाद बंद हो जाते। ये लोग अक्सर दिल्ली के रेडिओ स्टेशन , उर्दू बाजार के क़ुतुब खानों , दरिया गंज में बीसवीं सदी के अंसारी रोड ,आसिफ अली रोड के फुटपाथ या बैंचो पर या शमा के दफ्तर में मंडराते दिखाई देते। इन्हीं में से एक लेकिन सबसे अलबेले थे 'राजेंद्र मनचंदा बानी'। .
दिल्ली के कनॉट प्लेस की रौनक हुआ करता था रीगल सिनेमा हाल। सन 1932 में बना ये सिनेमा घर दिल्ली के सबसे लोकप्रिय सिनेमा घरों में से एक था जिसमें सिनेमा के अलावा ड्रामा, बैले, संगीत के कार्यक्रम, कला प्रदर्शनियां आदि भी हुआ करते थे । इसी सिनेमा घर के सामने एक रेलिंग हुआ करती थी, जिसके सहारे खड़े, झुके, टिके कवि, शायर, साहित्यकार, रंगकर्मी , चित्रकार याने आर्ट से जुडी सभी विधाओं के लोग बीड़ियाँ फूंकते और चाय सुड़कते हुए आपस में बहस करते देखे जा सकते थे।
अजीब तज़्रबा था भीड़ से गुजरने का
उसे बहाना मिला मुझसे बात करने का
थमा के एक बिखरता गुलाब मेरे हाथ
तमाशा देख रहा है वो मेरे डरने का
खड़े हों दोस्त कि दुश्मन सफ़ें सब एक ही हैं
वो जानता है, इधर से नहीं गुज़रने का
*
किसी चटान के अंदर उतर गया हूंँ मैं
कि अब मेरे लिए तूफाँ भी क्या, भंँवर भी क्या
*
फिर उसके हाथों हमें अपना क़त्ल भी था कुबूल
कि आ चुके थे क़रीब इतने, बच निकलते क्या
तमाम शहर था इक मोम का अजायबघर
चढ़ा जो दिन तो यह मंजर न फिर पिघलते क्या
*
कोई पहाड़ न दरिया न आग रस्ते में
अजब सपाट सफ़र है कि हादसा चाहूँ
*
आज तो रोने को जी हो जैसे
फिर कोई आस बंँधी हो जैसे
शहर में फिरता हूं तन्हा तन्हा
आशना एक वही हो जैसे
आशना परिचित
यासआलूद है एक एक घड़ी
ज़र्द फूलों की लड़ी हो जैसे
यासआलूद: निराशापूर्ण
भारी जिस्म और कद दरमियाना से थोड़ा कम के 'बानी' दिल्ली की शरणार्थी कॉलोनी राजेंद्र नगर में रहते थे ,मुल्तानी लहज़े में बड़े पुर सुकून अंदाज़ से पंजाबी बोलते। अभी वो रीगल सिनेमा की रेलिंग से टिक कर जिससे बात कर रहे हैं उनका नाम है मख़्मूर सईदी। दोनों सड़क से गुज़रती एक दरवाज़े वाली हर लाल बस से रीगल के सामने उतरने वाले इंसान को बड़े गौर से देख रहे हैं. आखिर एक शख़्स को उतरते देख दोनों के चेहरे खिल उठे 'बानी' जोर से आवाज़ दे कर बोले ओये 'कुमार पाशी ऐद्दर आजा ओये'। 'पाशी' ने दोनों को देख हाथ हिलाया तभी एक स्कूटर वाला तेज़ी से उसके सामने से गुज़रा। पाशी ने उसे हसरत से देखते हुए कहा यार 'बानी' हमारे पास कब स्कूटर होगा ? इस सवाल का जवाब बानी के पास नहीं था। 'स्कूटर न सही यार चाय तो मिल ही सकती है' पाशी मुस्कुराते हुए बोले। 'मख़्मूर' साहब ने हँसते हुए कहा 'हाँ क्यों नहीं इतनी औकात तो है अपनी मगर सुरेंद्र प्रकाश और राज नारायण'राज़' भी आ जाएँ फिर मिल के पीते हैं। ये पाँचों उर्दू के बड़े लेखक थे और तकरीबन रोज़ मिलते। यूँ समझो दांत काटे की रोटी थी इनकी दोस्ती। अक्सर सभी मिल कर कभी ज़फर इक़बाल तो कभी अहमद मुश्ताक़ की ग़ज़लों पर चर्चा करते। बानी यारों के यार थे। एक मुकम्मल इंसान ,सबकी इज़्ज़त करने वाले। एक संभली हुई शख़्सियत के मालिक।
कौन था मेरे पर तोलने पर नज़र किसकी थी
जिसने सर पर मेरे आस्माँ रख दिया, कौन था
*
कोई खड़ा है मेरी तरह भीड़ में तन्हा
नज़र बचा के मेरी सिम्त देखता है बहुत
ज़रा छुआ था कि बस पेड़ आ गिरा मुझ पर
कहांँ ख़बर थी कि अंदर से खोखला है बहुत
*
अदा ये किस कटे पत्ते से तूने सीखी है
सितम हवा का हो और शाख़ से शिकायत कर
नहीं अजब इसी पल का हो मुंतज़िर वो भी
कि छूले उसके बदन को, ज़रा सी हिम्मत कर
*
मुझे बिछड़ने का गम तो रहेगा हमसफ़रो
मगर सफ़र का तक़ाज़ा जुदा है मेरे लिए
*
वो मेरी ज़िन्दादिली का जाने क्या मांगे हिसाब
जाता मौसम है, कोई पत्ता हरा लेता चलूँ
*
टोक के जाने क्या कहता वो
उसने सुना सब बेध्यानी में
याद तेरी जैसे कि सरे शाम
धुंँध उतर जाए पानी में
आखिर सोचा देख लीजिए
क्या करता है वो मनमानी में
12 नवम्बर 1932 को मुल्तान ,अब पाकिस्तान,में जनाब गोबिंद राम मनचंदा के यहां राजिंदर जी का जन्म हुआ। मुल्क़ के बटवारे के कारण वो 1947 में दिल्ली आ गए और पंजाब यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स विषय में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। गुज़र बसर के लिए दिल्ली के एक स्कूल, जो डेरा इस्माइल खां से आकर बसे शरमार्थियों ने चला रखा था, में बच्चों को इकोनॉमिक्स पढ़ाते और खाली वक्त में शायरी करते। बानी की माली हालत कभी बहुत अच्छी नहीं रही लेकिन उनका रहन-सहन बहुत सलीकेदार रहा। आम शायरों की तरह न उनके पहनावे में और और न ही बातचीत में बिखराव था।
'बानी' की ज़िन्दगी और शायरी दोनों ने उनके साथ इंसाफ़ नहीं किया। ज़िन्दगी मुश्किल हालातों में गुज़री और शायरी ने उन्हें वो मुक़ाम नहीं दिलवाया जिसके सच्चे हक़दार थे। रिश्तेदारों और दोस्तों ने भी उनका साथ नहीं दिया। इतना कुछ होने के बावज़ूद बानी ने कभी इस बात का गिला किसी से नहीं किया। वो बाहर से हँसते रहे और अंदर से घुलते रहे। नतीज़ा, छोटी उम्र में ही उन्हें बीमारियों ने खोखला करना शुरू कर दिया। गठिया और गुर्दे के रोग उनके शरीर को बेशक कमज़ोर करते रहे लेकिन उनके चेहरे की मुस्कराहट को कभी कम नहीं कर पाये। यही कारण था की जब 11 अक्टूबर 1981 को मात्र 49 वर्ष की उम्र में दिल्ली के होली फैमली हॉस्पिटल से उनके मौत की ख़बर आयी तो लोगों को समझ ही नहीं आया कि देखने में अच्छा ख़ासा कसरती बदन वाला इंसान यूँ इस दुनिया से अचानक कैसे रुख़्सत हो गया।
कुछ न कुछ साथ अपने ये अंधा सफ़र ले जाएगा
पांँवों में ज़ंजीर डालूंगा तो सर ले जाएगा
घूमता है शहर के सबसे हसीं बाज़ार में
इक अज़ीयत नाक महरूमी वो घर ले जाएगा
*
सितम ये देख कि खुद मोतबर नहीं वो निगाह
कि जिस निगाह में हम मुस्तहक़ सज़ा के हैं
मोतबर :भरोसेमंद , मुस्तहक़: हक़दार
*
कोई क्या जानता क्या चीज़ किस पर बोझ है बानी
ज़रा सी ओस यूंँ तो सीनए-पत्थर प रक्खी थी
*
क्या तमाशा है कि हमसे इक क़दम उठता नहीं
और जितने मरहले बाकी हैं, आसानी के हैं
मरहले: पढ़ाव
ऐ दोस्त मैं ख़ामोश किसी डर से नहीं था
क़ाइल ही तिरी बात का अंदर से नहीं था
क़ाइल ही तिरी बात का अंदर से नहीं था
*
ओस से प्यास कहाँ बुझती है
मूसलाधार बरस मेरी जान
*
वो एक अक्स कि पल भर नज़र में ठहरा थातमाम उम्र का अब सिलसिला है मेरे लिए
*
आज क्या लौटते लम्हात मयस्सर आए
याद तुम अपनी इनायात से बढ़ कर आए
याद तुम अपनी इनायात से बढ़ कर आए
बानी साहब ने अपनी ज़िन्दगी में खूब लिखा जो पूरा नहीं छप पाया। उनकी ग़ज़लें और नज़्में उर्दू में जिन किताबों में छपी हैं उनके नाम हैं 'हर्फ़-ऐ-मोतबर' (1971 ), हिसाब-ऐ-रंग (1976 ), और शफ़क़ शजर (1982 ) . उन्होंने 'तलाश' नाम की एक मासिक पत्रिका भी निकाली जो आर्थिक तंगी के कारण बंद हो गयी लेकिन उसके सभी अंक बहुत चर्चित हुए। 'तलाश' में उन्होंने अपने समकालीन नए और स्थापित शायरों को छापा। उनकी बहुत सी अप्रकाशित रचनाएँ दिल्ली में उनके बेटे श्री विपिन बानी जी के पास सुरक्षित हैं जिन्हें वो शायद जल्द ही प्रकाशित करवाएं।
उनके समकालीन शायर जनाब निदा फ़ाज़ली ने उन्हें एक बार लिखा कि ' बानी तुम्हारी ग़ज़लें और नज़्में क्लासिक हैं जिनमें नए सिम्बोलिस्मों का प्रयोग इंसानी सोच को झिंझोड़ देता है। तुम्हारा अपना एक अलग स्टाईल है जो सबसे अलग है और ये बहुत बड़ी बात है। मैं तुम्हारी ग़ज़लें नज़्में हमेशा पढता रहता हूँ और जी खोल कर दाद देता हूँ। तुम्हारी तीखी सूझबूझ का मैं क़ायल हूँ।'
बशीर बद्र साहब ने जो बानी जी के दोस्त थे एक जगह लिखा है कि 'बानी --मैं रिसालों में बानी की मुहब्बत से डर कर छपता हूँ। अपने बुत और तुम्हारे ख़ुदा की क़सम मेरी दिली आरज़ू है कि जब मैं थका हारा आऊँ तो दो लम्हे तुम्हारे पास बैठ लूँ अपने इस यार से दिल की बातें करुँ जो मेरी तरह आँसू ,शबनम, पत्थर लफ़्ज़ों में जमा करता है। मुबारक हो दोस्त तुम इन दिनों क्या खूब कह रहे हो ज्यादा भी और अच्छा भी। बानी तुम नज़्म लिखो या ग़ज़ल तुम्हारा हर सुखन इक मक़ाम से होता है। मैं तुम्हारा यार हूँ अगर तुम्हारा कोई दुश्मन हो तो उससे पूछ कर देखो तुम्हारे क़लाम का वो भी आशिक़ निकलेगा। बानी तुम बहुत प्यारे इंसान और शायर हो।'
प्रोफ़ेसर शमीम हनफ़ी साहब का यू ट्यूब पर एक वीडिओ है जिसमें उन्होंने बानी साहब की शायरी पर रौशनी डाली है। वक़्त निकाल आप उसे सुनें।
'बानी' ज़रा सँभल के मोहब्बत का मोड़ काट
इक हादसा भी ताक में होगा यहीं कहीं
*
जाने वो कौन था और किस को सदा देता था
उस से बिछड़ा है कोई इतना पता देता था
*
मोहब्बतें न रहीं उस के दिल में मेरे लिए
मगर वो मिलता था हँस कर कि वज़्अ-दार जो था
वज़्अ-दार: सुरुचिपूर्ण
*
इस क़दर ख़ाली हुआ बैठा हूँ अपनी ज़ात में
कोई झोंका आएगा जाने किधर ले जाएगा
*
इस अँधेरे में न इक गाम भी रुकना यारो
अब तो इक दूसरे की आहटें काम आएँगी
*
वो हँसते खेलते इक लफ़्ज़ कह गया 'बानी'
मगर मिरे लिए दफ़्तर खुला मआनी का