बारहा ऐसा हुआ है याद तक दिल में न थी
बारहा मस्ती में लब पर उनका नाम आ ही गया
***
खाइयेगा इक निगाहे-लुत्फ़ का कब तक फ़रेब
कोई अफसाना बना कर बदगुमाँ हो जाइये
***
फिर मिरी आँख हो गयी नमनाक
फिर किसी ने मिज़ाज पूछा है
नमनाक =नम
***
कुछ तुम्हारी निगाह काफ़िर थी
कुछ मुझे भी खराब होना था
***
इश्क़ का ज़ौके-नज़ारा मुफ़्त में बदनाम है
हुस्न ख़ुद बेताब है जलवे दिखाने के लिए
ज़ौके-नज़ारा =देखने की चाह
***
मये-गुलफ़ाम भी है ,साज़े-इशरत भी है साक़ी भी
मगर मुश्किल है आशोबे-हक़ीक़त से गुज़र जाना
मये-गुलफ़ाम=फूल जैसी सुंदर शराब, साजे-इशरत =सुख संगीत,आशोबे-हक़ीक़त=वास्तविकता की पीड़ा
***
हुस्न को कर न दे ये शर्मिंदा
इश्क से ये ख़ता भी होती है
***
मुझे आज साहिल पे रोने भी दो
कि तूफ़ान में मुस्कुराना भी है
***
छलकती है जो तेरे जाम से उस मय का क्या कहना
तिरे शादाब होठों की मगर कुछ और है साकी
***
आँख से आँख जब नहीं मिलती
दिल से दिल हमकलाम होता है
जो लोग उर्दू शायरी से वाकिफ़ हैं उन्हें तो इन शेरों को पढ़ कर शायर के नाम का अंदाज़ा हो ही गया होगा लेकिन जो सिर्फ रस्मन शायरी से मोहब्बत करते हैं उन्हें शायद अभी तक कुछ पता न चला हो। कोई बात नहीं आखिर हम किस मर्ज़ की दवा हैं ? हम बताते हैं, लेकिन थोड़ी देर में। आपने ऊपर शेर पढ़े ही होंगे ,ज़ाहिर सी बात है ऐसे बेमिसाल शेर कहने वाले को सुनने वाले भी खूब मिलते होंगे। ये तब की बात है जब सोशल मिडिया का कुछ अता-पता नहीं था. कुछ लोग दोस्ती का वास्ता देकर उनसे सुनते होंगे तो कुछ उन्हें शराब पिला कर। 5 दिसम्बर 1955 की भयंकर सर्दी वाली इस मनहूस रात में शराबखाने की छत पे जो लोग इस शायर को घेर कर बैठे हैं वो इनके दोस्त नहीं हैं सिर्फ सुनने वाले हैं जो इन्हें शराब के एक के बाद दूसरा जाम पिला रहे हैं और बदले में इनसे दिलकश शेर और जबरदस्त जुमले सुन सुन कर खुश हो रहे हैं, तालियाँ बजा रहे हैं। रात गहरा रही है ठंडी हवा के साथ ओस भी गिरनी शुरू हो गयी है और शराब भी ख़तम हो चली है लिहाज़ा ये लोग एक एक करके धीरे धीरे वहां से खिसक रहे हैं , दोस्त होते तो वहां ठहरते और शायर को अपने साथ ले जाते लेकिन तमाशबीनों को सिर्फ तमाशे से मतलब होता है तमाशा दिखने वाले से नहीं। एक आध ने यूँ ही पूछ लिया मियाँ घर नहीं चलोगे तो जवाब मिला कि प्याले में कुछ बूँदें बची हैं हलक़ से उतार लें तो चलेंगे , कब प्याले की शराब ख़तम हुई और कब शराब के नशे ने पीने वाले को अपने आगोश में लिया किसी को ख़बर नहीं। शायर उस ठंडी रात को एक फटी पुरानी अचकन और ढीला ढाला पायजामा पहने शराबखाने की छत पर तनहा पड़ा रहा। सुबह जब उसे किसी ने देखा तो वो अकड़ा पड़ा था ,उसे तुरंत हस्पताल पहुँचाया गया लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।शायर के दिमाग की नस फट गयी थी।
शराब और इश्क़ ये दो ऐसी महामारियां हैं जिन्होंने किसी भी दूसरी बीमारी से ज्यादा शायरों की जान ली है। और दूसरी बिमारियों का तो फिर भी इलाज़ संभव है लेकिन इन दो में से किसी भी एक बीमारी से बच निकला थोड़ा मुश्किल है और कहीं ये दोनों एक साथ हो जाएँ तो फिर बचना ना-मुमकिन है. आप इतिहास उठा कर देखें तो पाएंगे कि ज़्यादातर शायरों या अति संवेदनशील लोगों को ये दोनों बीमारियां पता नहीं क्यों एक साथ ही होती हैं ? शराब और इश्क़ दोनों ही कभी आपको पूरी तरह तृप्त नहीं कर पाते इसीलिए एक अधूरापन एक प्यास हमेशा ज़ेहन में रहती है और यही कारण है कि इनकी गिरफ़्त में आया इंसान फिर बाहर नहीं आ पाता। इस अधूरेपन को पूरा करने की चाह में खुद पूरा हो जाता है। ये विषय व्यापक है इसलिए यहाँ चर्चा योग्य नहीं है ,इसे यहीं छोड़ते हैं और वापस अपने शायर की और लौटते हैं जो अब 'है' से 'था' में बदल चुका है। इंसान दरअस्ल मृतकों को पूजता है। सारी दुनिया में अधिकतर मौकों पर देखा गया है कि जब कोई इंसान मौजूद है तो उसके काम को न सराहना मिलती है न तवज्जोह लेकिन उसके इस दुनिया से रुख़्सत होते ही हमें अचानक उसमें छुपे सारे गुण बल्कि कुछ ऐसे गुण भी जो शायद उसमें थे ही नहीं, नज़र आने लगते हैं।कल तक जिसका नाम लेने में हमारी ज़बान लड़खड़ाने लगती थी उसके जाते ही हम उसी ज़बान से उसकी शान में कसीदे पढ़ने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है ? ऐसा कब तक होता रहेगा -पता नहीं। हमारे शायर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।
चलिए बात वहां से शुरू करते हैं जहाँ से शुरू होनी चाहिए याने फैज़ाबाद के रुदौली कस्बे से जहाँ के चौधरी सिराज उल हक़ के यहाँ 19 अक्टूबर 1911 को जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम रक्खा गया असरार उल हक़। सिराज उल हक़ उस इलाक़े के पहले ज़मींदार थे जिन्होंने वक़ालत जैसी उच्च शिक्षा प्राप्त की और ज़मींदारी पर सरकारी नौकरी को तरज़ीह दी। परिवार में जहाँ पुराने नियम कायदे माने जाते थे वहीँ नयी सोच को भी अपनाया जाता था। प्राथमिक शिक्षा के बाद हर पढ़े लिखे बाप की तरह सिराज साहब की तमन्ना थी कि असरार इंजीनियर बने लिहाज़ा उन्होंने असरार को आगरा के सेंट जांस कॉलेज में साइंस पढ़ने भेज दिया। अब साहब यूँ तमन्नाएँ पूरी होने लगें तो हर बाप का बेटा इंजिनियर डॉक्टर तो क्या टाटा बिरला अम्बानी न बन जाये ? आप लाख कोशिश करें होता वही है जो मंज़ूर-ए-खुदा होता है।'असरार' आगरा आ तो गए लेकिन दोस्ती कर बैठे फानी बदायूनी, जज़्बी और मैकश अकबराबादी जैसे शायरों से। बस फिर क्या था शायरी के कीड़े ने तो उन्हें काटा ही साथ ही शराब का भी चस्का लग गया। इंजीनियरिंग की पढाई धरी की धरी रह गयी, हज़रत साइंस में फेल हो गये। पिता, जिनका ट्रांसफर तब अलीगढ़ हो गया था, ने जब ये सुना तो अपना सर पीट लिया और असरार को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवा दिया वो भी आर्ट्स में। असरार को जैसा माहौल चाहिए था वैसा ही अलीगढ आ कर मिला और उनका शायरी का हुनर निखरने लगा। इस शहर में उनका राब्ता मंटो, इस्मत चुगताई, अली सरदार जाफ़री, सिब्ते हसन, जाँ निसार अख़्तर जैसे नामचीन शायरों से हुआ।यहीं उन्होंने अपना तख़ल्लुस 'शहीद' से बदल कर 'मजाज़' रख लिया। आज हम प्रकाश पंडित साहब द्वारा सम्पादित किताब 'मजाज़' आप के सामने ले आये हैं।
अलीगढ़ के गर्ल्स कॉलेज में उनकी ग़ज़लों और नज़्मों को तकिये के नीचे रख कर सोने वाली लड़कियों की तादाद भी कोई कम नहीं थी.अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मजाज़ के कलाम की तूती बोलने लगी। गर्ल्स कॉलेज से उन्हें बुलावे आते वो जाते, तब उनके और लड़कियों के बीच एक पर्दा तान दिया जाता, जिसके पार मजाज़ अपना कलाम तरन्नुम से पढ़ते और लड़कियां चूँकि उन्हें देख नहीं पाती थीं लिहाज़ा उनका अपने ज़ेहन में तसव्वुर करतीं और आहें भरतीं। शायरी सुनाने के बाद लड़कियां उनको वापस जाते हुए क्लास की खिड़कियों से देखतीं और दूर से बलाएँ लेतीं। मजाज़ की शख़्शियत ही ऐसी थी कि जिसे देख कर उन पर कुर्बान होने को दिल करे। बचपन में, जैसा की बहन "हमीदा" ने एक जगह लिखा है, "'मजाज़' बड़े सरल स्वभाव का निर्मल हृदय का व्यक्ति था | जागीरी वातावरण में स्वामित्य की भावना माँ के दूध के साथ मिलती है परन्तु मजाज़ में इस तरह का कोई भाव नहीं था | दूसरों की चीज को अपने प्रयोग में नहीं लाना और अपनी चीज दूसरों को दे देना उसकी आदत रही | इस के अतिरिक्त वह शुरू से ही सौंदर्य प्रेमी भी था | कुटुंब में कोई सुन्दर स्त्री देख लेता तो घंटो उसके पास बैठा रहता | खेल कूद, खाने पीने तक की सुध नहीं रहती।
मजाज़ की इश्किया शायरी अलीगढ़ में ज्यादा नहीं चल पायी क्यूंकि जल्द ही वो डॉ. अशरफ, मख़्दूम ,अख्तर रायपुरी, सबत हसन, सरदार जाफ़री, जज्बी और ऐसे दूसरे समाजवादी साथियों और इंकलाबी तरक्की पसंद शायरों की सोहबत में शामिल हो गये। ऐसे माहौल में मजाज ने ’इंकलाब’ जैसी नज्म बुनी। मजाज़ उन चंद शायरों में शामिल हैं जिन्होंने आधुनिक उर्दू शायरी को एक नया मोड़ दिया है. तरक्कीपसंद शायरों के लिए मुहब्बत और माशूका की खूबसूरती के बयान से अधिक समाज में गैर-बराबरी और भेदभाव का मसला अधिक बड़ा था. यहाँ से मजाज़ की शायरी ने अलग सी करवट ली और उनकी मशहूरी अलीगढ़ की सीमाओं से निकल कर पूरे हिंदुस्तान में हो गयी। उन्हें उर्दू शायरी का कीट्स कहा जाने लगा। इन्हीं दिनों दिल्ली के ऑल इण्डिया रेडियो से एक पत्रिका निकालने का ऐलान हुआ और असिस्टेंट एडिटर की पोस्ट पर काम करने के लिए मजाज़ के पास इंटरव्यू का बुलावा आया। मजाज़ नौकरी करने की नियत से अलीगढ़ छोड़ दिल्ली चल दिए ,ये सं 1935 की बात है। ।
दिल्ली के इंटरव्यू में सफलता मिली और ऑल इण्डिया रेडियो की पत्रिका 'आवाज़' में उन्हें असिस्टेंट एडिटर की नौकरी मिल गयी। नौकरी तो एक साल ही चल पायी क्यूंकि पत्रिका के संपादक मंडल से उनकी बनी नहीं ,लेकिन दिल्ली में किसी के साथ शुरू हुआ इश्क मरते दम तक मजाज़ के साथ चिपका रहा। मजाज़ की शायरी के प्रशंसक दिल्ली में यूँ तो ढेरों थे लेकिन एक ख़ातून जिनका नाम - छोड़िये नाम में क्या रखा है -जो शादीशुदा थीं उन पर और उनकी की शायरी पर बुरी तरह से फ़िदा हो गयीं। उसके खाविंद शायर तो नहीं थे लेकिन काफी पैसे वाले बिजनेसमैन थे। खातून को मजाज़ और उनकी शायरी बेइंतिहा पसंद थी लेकिन इतनी भी नहीं कि वो अपना भरापूरा महल नुमा घर छोड़ कर मजाज़ की झोपड़ी में ज़िन्दगी गुज़ार देतीं. मजाज़ तो इस बात को समझते थे लेकिन उनका दिल नहीं। पत्रिका छोड़ने के बाद दिल्ली में रहने का कोई सबब तो था नहीं इसलिए वो खुद तो लखनऊ चले आये लेकिन दिल वहीँ दिल्ली में छोड़ आये। लखनऊ में मजाज़ दिन-रात उस दिल्ली वाली के तसव्वुर में खोये रहते और अपना ग़म शराब में घोल कर पीते रहते।मजाज़ की उस वक्त की गयी शायरी उर्दू की बेहतरीन इश्किया शायरी में शुमार होती है। उन्होंने अपने ग़म को ज़माने के ग़म से जोड़ दिया। शराब की लत इस कदर बढ़ी कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि मजाज़ शराब को नहीं, शराब मजाज़ को पी रही है। इतना सबकुछ होने के बावजूद मजाज़ की ज़िंदादिली हमेशा कायम रही। कॉफी हॉउस हो या शराब खाने, मजाज़ के दिलचस्प जुमलों और चुटकुलों को सुन सुन कर ,लोगों के ठहाकों से गूंजते रहते। ये शायरी और ज़िंदादिली ही उस मनहूस रात उनकी मौत की वज़ह बनी। 1939 में सिब्ते हसन ,सरदार जाफरी और मजाज़ ने मिलकर ’नया अदब’ का सम्पादन किया जो आर्थिक कठिनाईयों की वजह से ज्यादा दिन तक नहीं चल सका।
"नया अदब" पत्रिका के बंद होने के बाद मजाज़ सड़क पर थे. पिता की पेंशन से घर बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था इसलिए मजाज़ को एक लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन की नौकरी करनी पड़ी। नौकरी के साथ साथ शराब और शायरी दोनों चलते रहे .'अख़्तर शीरानी' 'मजाज़' साहब के पसंददीदा शायर थे। उनके अचानक हुए इन्तेकाल ने मजाज़ को पागल सा कर दिया था। वो दौर अजब दौर था जब शायरों में कमाल की दोस्ती और भाईचारा हुआ करता था कोई धड़ेबंदी नहीं होती थी सब एक दूसरे की दिल खोलकर तारीफ करते और मौका मिलने पर टांग भी खींचते। एक दूसरे के घर बेतकल्लुफी से ठहरते हंसी मज़ाक और संजीदा गुफ़्तगू करते। आज हमें ये सब सोच के जरूर हैरत होती है क्यूंकि आज के शायरों के बीच जो रस्साकशी चल रही है उस पर कुछ न कहा जाए तो ही बेहतर है। 'मजाज़' के दोस्तों में जैसा पहले बताया जोश मलीहाबादी, प्रकाश पंडित , जां निसार अख़्तर, साहिर लुधियानवी, सरदार ज़ाफ़री , फैज़ अहमद फैज़, फ़िराक गोरखपुरी सज़्ज़ाद ज़हीर, मंटो, कृशन चन्दर , इस्मत चुगताई जैसे लोग थे। जोश से उनकी दोस्ती बेमिसाल थी। इस सब दोस्तों के बावजूद मजाज़ तन्हा थे। अधूरे इश्क़ बल्कि एकतरफा इश्क़ ने उन्हें कहीं न छोड़ा। घरवालों द्वारा उनकी तन्हाई को कम करने की तमाम कोशिशें नाकामयाब रहीं। जो लोग कभी मजाज़ को अपना दामाद बनाने के लिए आगे पीछे घूमा करते थे वही उनसे कनारा कर गए। कौन एक शराबी और कड़के शायर के साथ अपनी बेटी का रिश्ता करता ?
मजाज़ को कभी किसी दुश्मन की जरुरत नहीं पड़ी उनकी दुश्मनी खुद अपने आप से ही रही। उन्हें दो बार नर्वस ब्रेकडाउन हुआ लेकिन घरवालों की तीमारदारी से वो ठीक हो गए। आखिरी दिनों में उनपर पागलपन के दौरे पड़ने लगे और उन्हें रांची के पागल खाने में भर्ती करवा दिया जहाँ उनकी मुलाकात मशहूर इंकलाबी शायर 'काज़ी नज़रुल इस्लाम ' से हुई वो भी वहीँ भर्ती थे। कहते हैं उन्होंने क़ाज़ी साहब को पहचान लिया और उनसे कहा कि आप ऐसे चुप क्यों हैं ? चलिए हम लाहौर चलते हैं जो अब विदेशी ज़मीन है लेकिन पागलखाने तो वहां भी होंगे ही।" दुनिया के दो सबसे ज़हीन और कमाल के लोग और दोनों ही पागलखाने में। बकौल हयातुल्ला अंसारी ' दिल में इक हूक उठती है कि काश ! जिस तरह हुआ ,उस तरह न होता। काश !! दुनिया इससे बेहतर होती !! काश!! वो ऐसी होती कि 'मज़ाज' उसमें जी सकता। जी सकता और हंस सकता और नग्में गा सकता '
फैज़ साहब ने मजाज़ पर लिखा है कि ' मजाज़ की इन्क़िलाबियत आम इंकलाबी शायरों से अलग है। आम इंकलाबी शायर इन्किलाब के मुताल्लिक गरजते हैं , ललकारते हैं , सीना कूटते हैं, इन्किलाब के मुताल्लिक गा नहीं सकते ---वो सिर्फ इन्किलाब की हौलनाकी को देखते हैं उसके हुस्न को नहीं पहचानते। ये इन्किलाब का प्रगतिशील नहीं प्रतिक्रियात्मक तसव्वुर है। मजाज़ सच्चे मायनों में प्रगतिशील शायर था' शब्दों के साथ असाधारण कौशल, अति-उत्तम छंद, एक साहित्यिक उपज जिसमें न सिर्फ़ प्रेम-लीला है बल्कि इंक़लाब का नारा भी है. ऐसे शायर का इस प्रकार यूँ अंधकार में खो जाना, हमारी चूक है. इसे साहित्य के साथ नाइंसाफी का नाम दीजिए, मजाज़ के साथ बेईमानी का, बात बराबर है. मजाज़ के इस दुनिया से रुख़्सत होने के 53 साल बाद भारत सरकार ने उनपर एक डाक टिकट जारी किया। 2016 में उनपर फीचर फिल्म भी बनी जो न बनती तो भी मजाज़ की लोकप्रियता पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अली सरदार ज़ाफ़री साहब द्वारा उन पर दूरदर्शन के लिए बनाया सीरियल 'कहकशां' जरूर देखा जा सकता है।
सुना है एक बार सिने स्टार नरगिस जो उनकी बहन सफ़िया की सहेली थीं उनसे मिलने आयी और ऑटोग्राफ मांगे - ये सच है -उस वक्त अदीबों की क़द्र हुआ करती थी, आज ये बात जरूर अजूबा लग सकती है -खैर ! उन्होंने नरगिस जो सफ़ेद दुपट्टा ओढ़े हुए थीं को ऑटोग्राफ दिया और अपनी मशहूर नज़्म की दो लाइने भी साथ में लिख दीं - "तिरे माथे पे ये आँचल बहुत ही ख़ूब है लेकिन , तू इस आँचल से इक परचम बना लेती तो अच्छा था". ये पूरी नज़्म तरक्कीपसंद शायरी की मिसाल बन चुकी है। आप को बताता चलूँ कि बाद में सफ़िया की शादी शायर जां निसार अख़्तर साहब से हुई जिनके बेटे जावेद अख़्तर साहब का नाम तो आप सब ने सुना ही होगा। जी हाँ !! मजाज़ पद्म भूषण जावेद अख़्तर साहब के मामू थे। एक बार पंडित नेहरू अलीगढ़ यूनिवर्सिटी तशरीफ़ लाये और पूछा की क्या अलीगढ यूनिवर्सिटी का अपना कोई तराना है ? वो किसी भी जवाब से संतुष्ट नहीं हुए ये बात जब मजाज़ तक पहुंची तो दूसरे ही दिन उन्होंने 'ये मेरा चमन ये मेरा चमन , मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ' लिखा जिसे वहां अब भी गाया जाता है।
मजाज़ जैसे शायर पर इतने कम शब्दों में नहीं लिखा जा सकता उन्हें पूरा जानने के लिए आपको उनका लिखा पढ़ना होगा। शबे ताब , आहंग और साज़े नौ उनकी चर्चित किताबें हैं. मजाज़ की पूरी ज़िंदगी इक अधूरी ग़ज़ल है , वो तमाम उम्र अपने ज़ख्मों से खेलते रहे। मजाज़ की ग़ज़लें तो कम हैं लेकिन उनकी नज़्में और गीत कमाल के हैं और ये सभी आपको इस किताब में जिसकी बात आज हम कर रहे हैं में मिलेंगे जिनमें 'आवारा' 'किस से मोहब्बत है' , 'इन्किलाब', 'मज़बूरियां', बोल! री धरती बोल ! 'रात और रेल' ! 'दिल्ली से वापसी ', नौजवान ख़ातून से ', और 'नन्ही पुजारिन ' बार बार पढ़ने लायक हैं। इस किताब का पेपर बैक संस्करण सं 2018 में राजपाल एंड संस्- 1590 मदरसा रोड, कश्मीरी गेट दिल्ली -110006 ने सं 2018 में प्रकाशित किया है। ये किताब अमेज़न से भी ऑन लाइन मंगवाई जा सकती है। चलते चलते उनकी एक ग़ज़ल के ये शेर और पढ़ते हैं :
मजाज़ साहब पर की गयी कोई बात उनकी इस अमर नज़्म के बिना पूरी नहीं हो सकती जिसे दुनिया भर के न जाने कितने गायकों ने अपने अपने अंदाज़ में इसे गाया है , पूरी नज़्म पढ़ने के लिए आप किताब खरीदिये , बानगी के लिए यहाँ पढ़िए :
कुछ तुझको ख़बर है हम क्या क्या ए शोरीशे-दौरां भूल गये
वो जुल्फें-परीशां भूल गये, वो दीदा-ए-गिरियां भूल गये
शोरीशे-दौरां=संसार के उपद्रव, जुल्फें-परीशां=बिखरे केश ,दीदा-ए-गिरियां=रोती आँखें
अब गुलसे नज़र मिलती ही नहीं अब दिल की कली खिलती ही नहीं
ऐ फ़स्लें- बहारां रुख़सत हो हम लुत्फ़े-बहारां भूल गये
सब का तो मुदावा कर डाला अपना ही मुदावा कर न सके
सब के तो गरेबाँ सी डाले अपना ही गरेबाँ भूल गये
मुदावा =इलाज़
शराब और इश्क़ ये दो ऐसी महामारियां हैं जिन्होंने किसी भी दूसरी बीमारी से ज्यादा शायरों की जान ली है। और दूसरी बिमारियों का तो फिर भी इलाज़ संभव है लेकिन इन दो में से किसी भी एक बीमारी से बच निकला थोड़ा मुश्किल है और कहीं ये दोनों एक साथ हो जाएँ तो फिर बचना ना-मुमकिन है. आप इतिहास उठा कर देखें तो पाएंगे कि ज़्यादातर शायरों या अति संवेदनशील लोगों को ये दोनों बीमारियां पता नहीं क्यों एक साथ ही होती हैं ? शराब और इश्क़ दोनों ही कभी आपको पूरी तरह तृप्त नहीं कर पाते इसीलिए एक अधूरापन एक प्यास हमेशा ज़ेहन में रहती है और यही कारण है कि इनकी गिरफ़्त में आया इंसान फिर बाहर नहीं आ पाता। इस अधूरेपन को पूरा करने की चाह में खुद पूरा हो जाता है। ये विषय व्यापक है इसलिए यहाँ चर्चा योग्य नहीं है ,इसे यहीं छोड़ते हैं और वापस अपने शायर की और लौटते हैं जो अब 'है' से 'था' में बदल चुका है। इंसान दरअस्ल मृतकों को पूजता है। सारी दुनिया में अधिकतर मौकों पर देखा गया है कि जब कोई इंसान मौजूद है तो उसके काम को न सराहना मिलती है न तवज्जोह लेकिन उसके इस दुनिया से रुख़्सत होते ही हमें अचानक उसमें छुपे सारे गुण बल्कि कुछ ऐसे गुण भी जो शायद उसमें थे ही नहीं, नज़र आने लगते हैं।कल तक जिसका नाम लेने में हमारी ज़बान लड़खड़ाने लगती थी उसके जाते ही हम उसी ज़बान से उसकी शान में कसीदे पढ़ने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है ? ऐसा कब तक होता रहेगा -पता नहीं। हमारे शायर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।
तुम्हीं तो हो जिसे कहती है नाखुदा दुनिया
बचा सको तो बचा लो, कि डूबता हूँ मैं
इस इक हिजाब पे सौ बेहिजाबियाँ सदके
जहाँ से चाहता हूँ, तुमको देखता हूँ मैं
हिजाब =पर्दा
बताने वाले वहीँ पर बताते हैं मंज़िल
हज़ार बार जहाँ से गुज़र चुका हूँ मैं
चलिए बात वहां से शुरू करते हैं जहाँ से शुरू होनी चाहिए याने फैज़ाबाद के रुदौली कस्बे से जहाँ के चौधरी सिराज उल हक़ के यहाँ 19 अक्टूबर 1911 को जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम रक्खा गया असरार उल हक़। सिराज उल हक़ उस इलाक़े के पहले ज़मींदार थे जिन्होंने वक़ालत जैसी उच्च शिक्षा प्राप्त की और ज़मींदारी पर सरकारी नौकरी को तरज़ीह दी। परिवार में जहाँ पुराने नियम कायदे माने जाते थे वहीँ नयी सोच को भी अपनाया जाता था। प्राथमिक शिक्षा के बाद हर पढ़े लिखे बाप की तरह सिराज साहब की तमन्ना थी कि असरार इंजीनियर बने लिहाज़ा उन्होंने असरार को आगरा के सेंट जांस कॉलेज में साइंस पढ़ने भेज दिया। अब साहब यूँ तमन्नाएँ पूरी होने लगें तो हर बाप का बेटा इंजिनियर डॉक्टर तो क्या टाटा बिरला अम्बानी न बन जाये ? आप लाख कोशिश करें होता वही है जो मंज़ूर-ए-खुदा होता है।'असरार' आगरा आ तो गए लेकिन दोस्ती कर बैठे फानी बदायूनी, जज़्बी और मैकश अकबराबादी जैसे शायरों से। बस फिर क्या था शायरी के कीड़े ने तो उन्हें काटा ही साथ ही शराब का भी चस्का लग गया। इंजीनियरिंग की पढाई धरी की धरी रह गयी, हज़रत साइंस में फेल हो गये। पिता, जिनका ट्रांसफर तब अलीगढ़ हो गया था, ने जब ये सुना तो अपना सर पीट लिया और असरार को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवा दिया वो भी आर्ट्स में। असरार को जैसा माहौल चाहिए था वैसा ही अलीगढ आ कर मिला और उनका शायरी का हुनर निखरने लगा। इस शहर में उनका राब्ता मंटो, इस्मत चुगताई, अली सरदार जाफ़री, सिब्ते हसन, जाँ निसार अख़्तर जैसे नामचीन शायरों से हुआ।यहीं उन्होंने अपना तख़ल्लुस 'शहीद' से बदल कर 'मजाज़' रख लिया। आज हम प्रकाश पंडित साहब द्वारा सम्पादित किताब 'मजाज़' आप के सामने ले आये हैं।
हंस दिए वो मेरे रोने पर मगर
उनके हंस देने में भी इक राज़ है
छुप गए वो साजे-हस्ती छेड़ कर
अब तो बस आवाज़ ही आवाज़ है
सारी महफ़िल जिसपे झूम उट्ठी 'मज़ाज''
वो तो आवाज़े-शिकस्ते-साज़ है
अलीगढ़ के गर्ल्स कॉलेज में उनकी ग़ज़लों और नज़्मों को तकिये के नीचे रख कर सोने वाली लड़कियों की तादाद भी कोई कम नहीं थी.अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मजाज़ के कलाम की तूती बोलने लगी। गर्ल्स कॉलेज से उन्हें बुलावे आते वो जाते, तब उनके और लड़कियों के बीच एक पर्दा तान दिया जाता, जिसके पार मजाज़ अपना कलाम तरन्नुम से पढ़ते और लड़कियां चूँकि उन्हें देख नहीं पाती थीं लिहाज़ा उनका अपने ज़ेहन में तसव्वुर करतीं और आहें भरतीं। शायरी सुनाने के बाद लड़कियां उनको वापस जाते हुए क्लास की खिड़कियों से देखतीं और दूर से बलाएँ लेतीं। मजाज़ की शख़्शियत ही ऐसी थी कि जिसे देख कर उन पर कुर्बान होने को दिल करे। बचपन में, जैसा की बहन "हमीदा" ने एक जगह लिखा है, "'मजाज़' बड़े सरल स्वभाव का निर्मल हृदय का व्यक्ति था | जागीरी वातावरण में स्वामित्य की भावना माँ के दूध के साथ मिलती है परन्तु मजाज़ में इस तरह का कोई भाव नहीं था | दूसरों की चीज को अपने प्रयोग में नहीं लाना और अपनी चीज दूसरों को दे देना उसकी आदत रही | इस के अतिरिक्त वह शुरू से ही सौंदर्य प्रेमी भी था | कुटुंब में कोई सुन्दर स्त्री देख लेता तो घंटो उसके पास बैठा रहता | खेल कूद, खाने पीने तक की सुध नहीं रहती।
लाख छुपते हो मगर छुप के भी मस्तूर नहीं
तुम अजब चीज़ हो, नज़दीक नहीं, दूर नहीं
मस्तूर =छुपे हुए
ज़ुर्रते-अर्ज़ पे वो कुछ नहीं कहते लेकिन
हर अदा से ये टपकता है कि मंज़ूर नहीं
हाय वो वक़्त कि जब बे-पिये मदहोशी थी
हाय ये वक़्त कि अब पी के भी मख़्मूर नहीं
मख़्मूर=नशा
मजाज़ की इश्किया शायरी अलीगढ़ में ज्यादा नहीं चल पायी क्यूंकि जल्द ही वो डॉ. अशरफ, मख़्दूम ,अख्तर रायपुरी, सबत हसन, सरदार जाफ़री, जज्बी और ऐसे दूसरे समाजवादी साथियों और इंकलाबी तरक्की पसंद शायरों की सोहबत में शामिल हो गये। ऐसे माहौल में मजाज ने ’इंकलाब’ जैसी नज्म बुनी। मजाज़ उन चंद शायरों में शामिल हैं जिन्होंने आधुनिक उर्दू शायरी को एक नया मोड़ दिया है. तरक्कीपसंद शायरों के लिए मुहब्बत और माशूका की खूबसूरती के बयान से अधिक समाज में गैर-बराबरी और भेदभाव का मसला अधिक बड़ा था. यहाँ से मजाज़ की शायरी ने अलग सी करवट ली और उनकी मशहूरी अलीगढ़ की सीमाओं से निकल कर पूरे हिंदुस्तान में हो गयी। उन्हें उर्दू शायरी का कीट्स कहा जाने लगा। इन्हीं दिनों दिल्ली के ऑल इण्डिया रेडियो से एक पत्रिका निकालने का ऐलान हुआ और असिस्टेंट एडिटर की पोस्ट पर काम करने के लिए मजाज़ के पास इंटरव्यू का बुलावा आया। मजाज़ नौकरी करने की नियत से अलीगढ़ छोड़ दिल्ली चल दिए ,ये सं 1935 की बात है। ।
ख़ुद दिल में रहके आँख से पर्दा करे कोई
हाँ लुत्फ़ जब है पाके भी ढूँढा करे कोई
तुमने तो हुक्मे-तर्के-तमन्ना सुना दिया
किस दिल से आह तर्के-तमन्ना करे कोई
मुझको ये आरज़ू वो उठाएं नक़ाब ख़ुद
उनको ये इन्तिज़ार तक़ाज़ा करे कोई
दिल्ली के इंटरव्यू में सफलता मिली और ऑल इण्डिया रेडियो की पत्रिका 'आवाज़' में उन्हें असिस्टेंट एडिटर की नौकरी मिल गयी। नौकरी तो एक साल ही चल पायी क्यूंकि पत्रिका के संपादक मंडल से उनकी बनी नहीं ,लेकिन दिल्ली में किसी के साथ शुरू हुआ इश्क मरते दम तक मजाज़ के साथ चिपका रहा। मजाज़ की शायरी के प्रशंसक दिल्ली में यूँ तो ढेरों थे लेकिन एक ख़ातून जिनका नाम - छोड़िये नाम में क्या रखा है -जो शादीशुदा थीं उन पर और उनकी की शायरी पर बुरी तरह से फ़िदा हो गयीं। उसके खाविंद शायर तो नहीं थे लेकिन काफी पैसे वाले बिजनेसमैन थे। खातून को मजाज़ और उनकी शायरी बेइंतिहा पसंद थी लेकिन इतनी भी नहीं कि वो अपना भरापूरा महल नुमा घर छोड़ कर मजाज़ की झोपड़ी में ज़िन्दगी गुज़ार देतीं. मजाज़ तो इस बात को समझते थे लेकिन उनका दिल नहीं। पत्रिका छोड़ने के बाद दिल्ली में रहने का कोई सबब तो था नहीं इसलिए वो खुद तो लखनऊ चले आये लेकिन दिल वहीँ दिल्ली में छोड़ आये। लखनऊ में मजाज़ दिन-रात उस दिल्ली वाली के तसव्वुर में खोये रहते और अपना ग़म शराब में घोल कर पीते रहते।मजाज़ की उस वक्त की गयी शायरी उर्दू की बेहतरीन इश्किया शायरी में शुमार होती है। उन्होंने अपने ग़म को ज़माने के ग़म से जोड़ दिया। शराब की लत इस कदर बढ़ी कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि मजाज़ शराब को नहीं, शराब मजाज़ को पी रही है। इतना सबकुछ होने के बावजूद मजाज़ की ज़िंदादिली हमेशा कायम रही। कॉफी हॉउस हो या शराब खाने, मजाज़ के दिलचस्प जुमलों और चुटकुलों को सुन सुन कर ,लोगों के ठहाकों से गूंजते रहते। ये शायरी और ज़िंदादिली ही उस मनहूस रात उनकी मौत की वज़ह बनी। 1939 में सिब्ते हसन ,सरदार जाफरी और मजाज़ ने मिलकर ’नया अदब’ का सम्पादन किया जो आर्थिक कठिनाईयों की वजह से ज्यादा दिन तक नहीं चल सका।
चारागरी सर आँखों पर इस चारागरी से क्या होगा
दर्द की अपनी आप दवा है , तुमसे अच्छा क्या होगा
वाइज़े-सादालौह से कह दो छोड़ उक़्वा की बातें
इस दुनिया में क्या रक्खा है, उस दुनिया में क्या होगा
वाइज़े-सादालौह से =सरल स्वाभाव वाले धर्मोदेशक से , उक़्वा=परलोक
तुम भी 'मज़ाज' इंसान हो आखिर लाख छुपाओ इश्क अपना
ये भेद मगर खुल जाएगा ये राज़ मगर अफ़शा होगा
अफ़शा=प्रकट
ये भेद मगर खुल जाएगा ये राज़ मगर अफ़शा होगा
अफ़शा=प्रकट
"नया अदब" पत्रिका के बंद होने के बाद मजाज़ सड़क पर थे. पिता की पेंशन से घर बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था इसलिए मजाज़ को एक लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन की नौकरी करनी पड़ी। नौकरी के साथ साथ शराब और शायरी दोनों चलते रहे .'अख़्तर शीरानी' 'मजाज़' साहब के पसंददीदा शायर थे। उनके अचानक हुए इन्तेकाल ने मजाज़ को पागल सा कर दिया था। वो दौर अजब दौर था जब शायरों में कमाल की दोस्ती और भाईचारा हुआ करता था कोई धड़ेबंदी नहीं होती थी सब एक दूसरे की दिल खोलकर तारीफ करते और मौका मिलने पर टांग भी खींचते। एक दूसरे के घर बेतकल्लुफी से ठहरते हंसी मज़ाक और संजीदा गुफ़्तगू करते। आज हमें ये सब सोच के जरूर हैरत होती है क्यूंकि आज के शायरों के बीच जो रस्साकशी चल रही है उस पर कुछ न कहा जाए तो ही बेहतर है। 'मजाज़' के दोस्तों में जैसा पहले बताया जोश मलीहाबादी, प्रकाश पंडित , जां निसार अख़्तर, साहिर लुधियानवी, सरदार ज़ाफ़री , फैज़ अहमद फैज़, फ़िराक गोरखपुरी सज़्ज़ाद ज़हीर, मंटो, कृशन चन्दर , इस्मत चुगताई जैसे लोग थे। जोश से उनकी दोस्ती बेमिसाल थी। इस सब दोस्तों के बावजूद मजाज़ तन्हा थे। अधूरे इश्क़ बल्कि एकतरफा इश्क़ ने उन्हें कहीं न छोड़ा। घरवालों द्वारा उनकी तन्हाई को कम करने की तमाम कोशिशें नाकामयाब रहीं। जो लोग कभी मजाज़ को अपना दामाद बनाने के लिए आगे पीछे घूमा करते थे वही उनसे कनारा कर गए। कौन एक शराबी और कड़के शायर के साथ अपनी बेटी का रिश्ता करता ?
बहुत मुश्किल है दुनिया का संवरना
तिरी जुल्फ़ों का पेचो-ख़म नहीं है
बहुत कुछ और भी है इस जहाँ में
ये दुनिया महज़ ग़म ही ग़म नहीं है
मिरी बर्बादियों का हम-नशीनों
तुम्हें क्या ख़ुद मुझे भी ग़म नहीं है
मजाज़ को कभी किसी दुश्मन की जरुरत नहीं पड़ी उनकी दुश्मनी खुद अपने आप से ही रही। उन्हें दो बार नर्वस ब्रेकडाउन हुआ लेकिन घरवालों की तीमारदारी से वो ठीक हो गए। आखिरी दिनों में उनपर पागलपन के दौरे पड़ने लगे और उन्हें रांची के पागल खाने में भर्ती करवा दिया जहाँ उनकी मुलाकात मशहूर इंकलाबी शायर 'काज़ी नज़रुल इस्लाम ' से हुई वो भी वहीँ भर्ती थे। कहते हैं उन्होंने क़ाज़ी साहब को पहचान लिया और उनसे कहा कि आप ऐसे चुप क्यों हैं ? चलिए हम लाहौर चलते हैं जो अब विदेशी ज़मीन है लेकिन पागलखाने तो वहां भी होंगे ही।" दुनिया के दो सबसे ज़हीन और कमाल के लोग और दोनों ही पागलखाने में। बकौल हयातुल्ला अंसारी ' दिल में इक हूक उठती है कि काश ! जिस तरह हुआ ,उस तरह न होता। काश !! दुनिया इससे बेहतर होती !! काश!! वो ऐसी होती कि 'मज़ाज' उसमें जी सकता। जी सकता और हंस सकता और नग्में गा सकता '
इक अर्ज़े-वफ़ा भी कर न सके, कुछ कह न सके, कुछ सुन न सके
यां हमने ज़बां ही खोली थी , वां आँख झुकी शरमा भी गए
रूदादे-ग़मे-उल्फ़त उनसे हम क्या कहते, क्योंकर कहते
इक हर्फ़ न निकला होठों से और आँख में आंसू आ भी गए
रूदादे-ग़मे-उल्फ़त=प्रेम के दुखों की कहानी
रूदादे-ग़मे-उल्फ़त=प्रेम के दुखों की कहानी
उस महफ़िले-कैफ़ों-मस्ती में, उस अंजुमने-इर्फ़ानी में
सब जाम-ब-कफ़ बैठे ही रहे, हम पी भी गए, छलका भी गए
अंजुमने-इर्फ़ानी में=ज्ञानियों की महफ़िल में ,जाम-ब-कफ़=प्याला हाथ में लिए
अंजुमने-इर्फ़ानी में=ज्ञानियों की महफ़िल में ,जाम-ब-कफ़=प्याला हाथ में लिए
फैज़ साहब ने मजाज़ पर लिखा है कि ' मजाज़ की इन्क़िलाबियत आम इंकलाबी शायरों से अलग है। आम इंकलाबी शायर इन्किलाब के मुताल्लिक गरजते हैं , ललकारते हैं , सीना कूटते हैं, इन्किलाब के मुताल्लिक गा नहीं सकते ---वो सिर्फ इन्किलाब की हौलनाकी को देखते हैं उसके हुस्न को नहीं पहचानते। ये इन्किलाब का प्रगतिशील नहीं प्रतिक्रियात्मक तसव्वुर है। मजाज़ सच्चे मायनों में प्रगतिशील शायर था' शब्दों के साथ असाधारण कौशल, अति-उत्तम छंद, एक साहित्यिक उपज जिसमें न सिर्फ़ प्रेम-लीला है बल्कि इंक़लाब का नारा भी है. ऐसे शायर का इस प्रकार यूँ अंधकार में खो जाना, हमारी चूक है. इसे साहित्य के साथ नाइंसाफी का नाम दीजिए, मजाज़ के साथ बेईमानी का, बात बराबर है. मजाज़ के इस दुनिया से रुख़्सत होने के 53 साल बाद भारत सरकार ने उनपर एक डाक टिकट जारी किया। 2016 में उनपर फीचर फिल्म भी बनी जो न बनती तो भी मजाज़ की लोकप्रियता पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अली सरदार ज़ाफ़री साहब द्वारा उन पर दूरदर्शन के लिए बनाया सीरियल 'कहकशां' जरूर देखा जा सकता है।
तुझी से तुझे छीनना चाहता हूँ
ये क्या चाहता हूँ ये क्या चाहता हूँ
ख़ताओं पे जो मुझको माइल करे फिर
सज़ा और ऐसी सज़ा चाहता हूँ
माइल =प्रवृत
तुझे ढूंढता हूँ तिरी जुस्तजू है
मज़ा है कि ख़ुद गुम हुआ चाहता हूँ
सुना है एक बार सिने स्टार नरगिस जो उनकी बहन सफ़िया की सहेली थीं उनसे मिलने आयी और ऑटोग्राफ मांगे - ये सच है -उस वक्त अदीबों की क़द्र हुआ करती थी, आज ये बात जरूर अजूबा लग सकती है -खैर ! उन्होंने नरगिस जो सफ़ेद दुपट्टा ओढ़े हुए थीं को ऑटोग्राफ दिया और अपनी मशहूर नज़्म की दो लाइने भी साथ में लिख दीं - "तिरे माथे पे ये आँचल बहुत ही ख़ूब है लेकिन , तू इस आँचल से इक परचम बना लेती तो अच्छा था". ये पूरी नज़्म तरक्कीपसंद शायरी की मिसाल बन चुकी है। आप को बताता चलूँ कि बाद में सफ़िया की शादी शायर जां निसार अख़्तर साहब से हुई जिनके बेटे जावेद अख़्तर साहब का नाम तो आप सब ने सुना ही होगा। जी हाँ !! मजाज़ पद्म भूषण जावेद अख़्तर साहब के मामू थे। एक बार पंडित नेहरू अलीगढ़ यूनिवर्सिटी तशरीफ़ लाये और पूछा की क्या अलीगढ यूनिवर्सिटी का अपना कोई तराना है ? वो किसी भी जवाब से संतुष्ट नहीं हुए ये बात जब मजाज़ तक पहुंची तो दूसरे ही दिन उन्होंने 'ये मेरा चमन ये मेरा चमन , मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ' लिखा जिसे वहां अब भी गाया जाता है।
क्यों जवानी की मुझे याद आई
मैंने इक ख़्वाब सा देखा क्या था
हुस्न की आँख भी नमनाक हुई
इश्क को आपने समझा क्या था
इश्क ने आँख झुका ली वरना
हुस्न और हुस्न का पर्दा क्या था
मजाज़ जैसे शायर पर इतने कम शब्दों में नहीं लिखा जा सकता उन्हें पूरा जानने के लिए आपको उनका लिखा पढ़ना होगा। शबे ताब , आहंग और साज़े नौ उनकी चर्चित किताबें हैं. मजाज़ की पूरी ज़िंदगी इक अधूरी ग़ज़ल है , वो तमाम उम्र अपने ज़ख्मों से खेलते रहे। मजाज़ की ग़ज़लें तो कम हैं लेकिन उनकी नज़्में और गीत कमाल के हैं और ये सभी आपको इस किताब में जिसकी बात आज हम कर रहे हैं में मिलेंगे जिनमें 'आवारा' 'किस से मोहब्बत है' , 'इन्किलाब', 'मज़बूरियां', बोल! री धरती बोल ! 'रात और रेल' ! 'दिल्ली से वापसी ', नौजवान ख़ातून से ', और 'नन्ही पुजारिन ' बार बार पढ़ने लायक हैं। इस किताब का पेपर बैक संस्करण सं 2018 में राजपाल एंड संस्- 1590 मदरसा रोड, कश्मीरी गेट दिल्ली -110006 ने सं 2018 में प्रकाशित किया है। ये किताब अमेज़न से भी ऑन लाइन मंगवाई जा सकती है। चलते चलते उनकी एक ग़ज़ल के ये शेर और पढ़ते हैं :
कभी साहिल पे रह कर शौक़ तूफानों से टकराएं
कभी तूफां में रह कर फिक्र है साहिल नहीं मिलता
ये आना कोई आना है कि बस रस्मन चले आए
ये मिलना ख़ाक मिलना है कि दिल से दिल नहीं मिलता
ये क़त्ले-आम और बे-इज़्न क़त्ले-आम कहिये
ये बिस्मिल कैसे बिस्मिल हैं जिन्हें क़ातिल नहीं मिलता
बे-इज़्न=बिना इजाज़त, बिस्मिल =घायल
मजाज़ साहब पर की गयी कोई बात उनकी इस अमर नज़्म के बिना पूरी नहीं हो सकती जिसे दुनिया भर के न जाने कितने गायकों ने अपने अपने अंदाज़ में इसे गाया है , पूरी नज़्म पढ़ने के लिए आप किताब खरीदिये , बानगी के लिए यहाँ पढ़िए :
शहर की रात और मैं नाशादो-नाकारा फिरूं
जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं
ग़ैर की बस्ती है कब तक दर-ब-दर मारा फिरूं
ऐ ग़मे -दिल क्या करूँ , ऐ वहशते-दिल क्या करूँ !






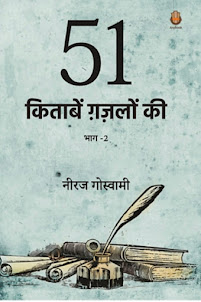







5 comments:
आपकी इस प्रविष्टि् के लिंक की चर्चा कल मंगलवार (27-11-2018) को "जिन्दगी जिन्दगी पे भारी है" (चर्चा अंक-3168) पर भी होगी।
--
चर्चा मंच पर पूरी पोस्ट नहीं दी जाती है बल्कि आपकी पोस्ट का लिंक या लिंक के साथ पोस्ट का महत्वपूर्ण अंश दिया जाता है।
जिससे कि पाठक उत्सुकता के साथ आपके ब्लॉग पर आपकी पूरी पोस्ट पढ़ने के लिए जाये।
--
हार्दिक शुभकामनाओं के साथ।
सादर...!
डॉ.रूपचन्द्र शास्त्री 'मयंक'
आपकी प्रस्तुतियों ने बहुत से शौकीनों को नायाब शायरी से मिलवाया है। समय निकालकर पुस्तक खरीदना, उसे पढ़ना और फिर उसे सरल भाषा में प्रस्तुत करना प्रशंसनीय है।
साधुवाद आपके प्रयत्नों के प्रति।
'मजाज' उर्दू शेरो शायरी को जानने, चाहने वालो के लिए मोहब्बत का वो खुदा है जिसे खुद मोहब्बत नसीब ना हो सकी भले ही उसने खुद कितने ही अश’आर और ग़ज़ल मोहब्बत पे लिख दी हो; असरार उल हक़ 'मज़ाज' ने भी ग़ालिब और ख़ुदा-ए-सुख़न मीर और दुष्यंत की उसी रवायत को आगे बढ़ाया जिसमे उन्हें जीते जी तो वो मशहूरी ना मिल सकी जिसके वो हक़दार थे पर उनके इंतकाल के बाद उनकी ग़ज़लों, नज़्मों को सर माथे बैठाया गया।
मैं मयकशी का शौक नहीं पालता ना ही कभी उसका इरादा किया; पर जब भी अपने मन पसंद शायरों के लिए पढ़ता हूँ की मयकशी उन्हें बर्बाद कर गयी तो बड़ा ही दुःख होता है चाहे वो ग़ालिब हो, जिगर हो या फिर मज़ाज ही ; काश ये मयकश ना होते तो
मज़ाज के लिए एक किस्सा मशहूर है; मज़ाज जरुरत से ज्यादा ही पीने लगे थे एक दिन जोश मलीहाबादी ने चिढ़ते हुए मज़ाज से कहा की 'मजाज़' तुम घड़ी रख कर पिया करो, मजाज़ ने छूटते ही ज़वाब दिया यहाँ घड़ी नहीं हम घड़ा रख कर पीते है, अब कर लो ऐसे इंसान का कुछ गर किया जा सकता हो तो
मज़ाज की शेरों शायरी किस वज़न की थी ये इसी बात से पता चल जाता है नेहरू जी के ये कहने पे की उन्हें इस बात पे विश्वास नहीं की इतनी बेहतरीन यूनिवर्सिटी का अपना कोई तराना नहीं है; मज़ाज ने रात भर बैठ कर एक बेहतरीन नज़्म लिखी जिसे मैंने ना जाने कितनी बार अपनी आँखों में आंसुओं के साथ सुना और गुनगुनाया है और जिसे मज़ाज के इंतकाल के बाद अलीगढ यूनिवर्सिटी ने अपने बुलबुल की इज़्ज़त फजाई के लिए मज़ाज की नज़्म 'ये मेरा चमन ये मेरा चमन , मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ' को तराना-ए-यूनिवर्सिटी बना दिया पर ये नज़्म भी मेरे जैसे इंसानो की पसंद है जिन्हे अपनी मिट्टी की याद आज भी है और जो आज भी उन जगहों से जुड़े है जंहा से वो पले बढे और लिखे पढ़े है।
चारागरी सर आँखों पर इस चारागरी से क्या होगा
दर्द की अपनी आप दवा है , तुमसे अच्छा क्या होगा
शायद इस शेर की तरह मज़ाज को भी जिंदगी भर अपनी दवा का ही इंतज़ार रह गया
शहर की रात और मैं नाशादो-नाकारा फिरूं
जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं
ग़ैर की बस्ती है कब तक दर-ब-दर मारा फिरूं
ऐ ग़मे -दिल क्या करूँ , ऐ वहशते-दिल क्या करूँ !
मज़ाज शायद खुद को ही अपनी गजलों और नज़्मों में सवारते और सजाते रहे और ये ग़ज़ल भी शायद उन्होंने अपनी आवारगी और मयकशी के लिए ही लिखी थी।
हमेशा की तरह एक बार फिर नीरज जी का शुक्रिया जो उन्होंने मेरी मनपसंद नज़्म के शायर से मेरी मुलाकात कराई।
फिर मेरी आँख हो गई नमनाक
फिर किसी ने मिज़ाज पूछा है
खूबसूरत तब्सिरे के लिए साधुवाद।
मोब 8383809043
Very nice article. I like your writing style. I am also a blogger. I always admire you. You are my idol. I have a post of my blog can you check this : Chennai super kings team
Post a Comment