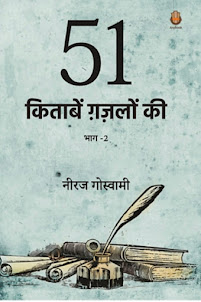हमने बौनों की जेब में देखी
नाम जिस चीज़ का सफलता है
तन बदलती थी आत्मा पहले
आजकल तन उसे बदलता है
एक धागे का साथ देने को
मोम का रोम रोम जलता है
उसका कुछ तो इलाज़ करवाओ
उसके व्यवहार में सरलता है
सीधे आम बोल चाल के शब्दों से गहरी बात करने में माहिर शायर बहुतायत में नहीं हैं. उन चंद नामवर शायरों में से एक जिनका नाम बहुत इज्ज़त से लिया जाता है शायर हैं हिंदी काव्य में अपनी मधुर गीतों के लिए प्रसिद्द श्री "बाल स्वरुप राही" साहब. ये ऐसी शख्शियत हैं जो किसी भी काव्य प्रेमी के लिए परिचय की मोहताज़ नहीं. आज हम उनकी पुस्तक " राही को समझाए कौन" का जिक्र करेंगे जिसे किताब घर प्रकाशन से प्रकाशित किया गया है.

हमें परहेज़ की बारीकियां समझाई जाती हैं
कि जब रंगीन शामों में खुली दावत के दिन आये
किसी महफ़िल, किसी जलवे, किसी बुत से नहीं नाता
पड़े हैं एक कोने में अजब फ़ुर्सत के दिन आये
बुजुर्गों में हमारा नाम भी शामिल हुआ शायद
बड़ी बदनामियों के बाद ये शोहरत के दिन आये
बुद्धिजीवी फिर इकठ्ठे हो गए
फिर ज़रूरी प्रश्न टाले जायेंगे
जिनकी कोशिश है कि कुछ बेहतर करें
नाम उनके ही उछाले जायेंगे
मिल गया राही सचाई का सिला
पेट में सूखे निवाले जायेंगे
प्रो.सादिक़ साहब इस किताब की भूमिका में लिखते हैं "राही साहब ने 1953 के आसपास जब ग़ज़ल / कविता लेखन शुरू किया तब कविता के नाम पर बहुत से प्रयोग हो रहे थे और लय बद्ध या छंद बद्ध कविताओं का बड़ी शिद्दत के साथ तिरस्कार किया जा रहा था , गीत और ग़ज़ल जैसी काव्य विधाओं को निरर्थक, निष्फल और अनुचित मानकर हिक़ारत की नज़र से देखा जाने लगा था लेकिन राही साहब पूरी संजीदगी से इन्हें अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाये रहे. ये अमल अपने और अपनी कला -क्षमता पर पूर्ण विशवास के बगैर संभव नहीं." सादिक़ साहब की बात इस किताब को पढ़ते वक़्त पूरी तरह खरी उतरती मालूम होती है:
हम पर दुःख का परबत टूटा तब हमने दो चार कहे
उस पे भला क्या बीती होगी जिसने शेर हज़ार कहे
अब किसके आगे हम अपना दुखड़ा रोयें छोड़ो यार
एक बात को आखिर कोई बोलो कितनी बार कहे
ढूंढ रहे हो गाँव गाँव में जा कर किस सच्चाई को
सच तो सिर्फ वही होता है जो दिल्ली दरबार कहे
आईये अब उनकी एक छोटी बहर की ग़ज़ल के कुछ शेरों पर नज़र डालें:-
रोटी सेक रहा है कौन
सारा शहर बना तंदूर
झूठ के जैसे तानाशाह
सच जैसे बंधुआ मज़दूर
सच जैसे बंधुआ मज़दूर
इसका कोई नहीं इलाज़
स्वाभिमान ऐसा नासूर
राही को समझाए कौन
कविताई है सिर्फ फितूर
लगे जब चोट सीने में ह्रदय का भान होता है
सहे आघात जो हंस कर वही इंसान होता है
लगाकर कल्पना के पर उड़ा करते सभी नभ पर
शिला से शीश टकरा कर मुझे अभिमान होता है
पहचान अगर बन न सकी तेरी तो क्या ग़म
कितने ही सितारों का कोई नाम नहीं है
मत सोच कि क्या तूने दिया तुझको मिला क्या
शायर है जमा-ख़र्च तेरा काम नहीं है
उठने दे जो उठता है धुआं दिल की गली से
बस्ती वो कहाँ है जहाँ कोहराम नहीं है
टपकेगा रुबाई से तेरी ख़ून या आंसू
राही है तेरा नाम तू खैयाम नहीं है