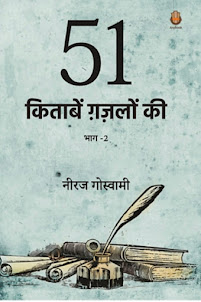किताब खरीदते वक्त एक बात ज़ेहन में रहती है जो पता नहीं कब किसने कही लेकिन साहब खूब कही कि
"एक अच्छी किताब १०० दोस्तों के बराबर होती है, लेकिन एक अच्छा दोस्त पुस्तकालय के बराबर होता है, ईश्वर ने हमें माँ, बाप, भाई, बहन और दूसरे रिश्तेदार चुनने की आजादी नही दी है, लेकिन एक अच्छा दोस्त चुनने की आजादी दी है, आइए अच्छे दोस्त बनाएँ!" दोस्त तो किस्मत से मिलते हैं लेकिन किताबें खोजने से मिल जाती है. दोस्तों के पीठ पीछे से वार करने की कला का उर्दू शायरी में खूब बखान किया गया है लेकिन कभी किसी किताब ने आपसे दगाबाजी की हो ये कभी कहीं कहा गया.
आज की किताब के शायर एक ऐसी शाख्यियत हैं जिनके बारे में बहुत कम पढ़ा सुना गया है. आज के दौर के पाठकों की तो बात ही छोडिये हमारे ज़माने के लोग भी, जो शायरी में थोड़ी बहुत दखल रखते हैं, इनका नाम सुन कर हो सकता है अपना सर खुजलाने लगें. कुछ ऐसे बदनसीब शायर होते हैं जो अपनी ज़िन्दगी में वो मकबूलियत हासिल नहीं कर पाते जो उन्हें मरने के बाद नसीब होती है. वैसे भी गुज़रे वक्त और गुज़रे इंसानों की वंदना हमारे खून में है.
कुछ खास दोस्त अक्सर मुझे कहते हैं कि यार तुम अपनी भूमिका में पकाते बहुत हो सीधे सीधे मुद्दे पर क्यूँ नहीं आते, उन्हें मैं हंस कर जवाब देता हूँ के भाई क्या करूँ ये मुझ पर टी.वी. सीरियलस देखने के शौक का असर है, जो सालों चलने के बावजूद भी असली मुद्दे पर नहीं आते. मजाक को यहीं छोड़ चलिए मुद्दे पर आते हैं:-
आ के पत्थर तो मेरे सहन में दो चार गिरे
जितने उस पेड़ के फल थे पस-ए-दीवार गिरे
(सहन: आँगन , पस-ऐ-दीवार: दीवार के पीछे)
मुझे गिरना है तो मैं अपने ही क़दमों में गिरुं
जिस तरह साया-ए-दीवार पे दीवार गिरे
क्या कहूँ दीदा-ए-तर ये तो मिरा चेहरा है
संग कट जाते हैं बारिश की जहाँ धार गिरे
दीदा-ए-तर : आंसू भरी आँखें, संग : पत्थर
देखते क्यूँ हो 'शकेब' इतनी बलंदी की तरफ
न उठाया करो सर को कि ये दस्तार गिरे
दस्तार: पगड़ी
"मुझे गिरना है तो मैं अपने ही क़दमों में गिरुं " जैसे खुद्दारी से भरे मिसरे लिखने वाले इस शायर का नाम है जनाब
"शकेब जलाली" साहब जो 1अक्तूबर 1934 को अलीगड़ के पास एक छोटे से गाँव सद्दत में पैदा हुए और 12 नवम्बर 1966 को याने सिर्फ बत्तीस साल की कम उम्र में इस दुनिया ऐ फानी से रुखसत हो गए. आज इसी शायर की अनमोल शायरी के पहले हिंदी संकलन
"दरख़्त पानी के" का जिक्र करेंगे जिसे डायमंड बुक्स वालों ने प्रकाशित किया है.

उतर के नाव से भी कब सफ़र तमाम हुआ
ज़मीं पे पाँव धरा तो ज़मीन चलने लगी
जो दिल का ज़हर था काग़ज़ पर सब बिखेर दिया
फिर अपने आप तबियत मिरी संभलने लगी
जहाँ शज़र पे लगा था तबर का ज़ख्म 'शकेब'
वहीँ पे देख ले कोंपल नयी निकलने लगी
तबर: फरसा, कुल्हाड़ी
'शकेब जलाली' जी ने महज़ पंद्रह साल की उम्र से ग़ज़ल कहना शुरू कर दिया था . उन्होंने उर्दू शायरी को नयी दिशा दी जिसे उनके साथ के और बाद के नामचीन शायरों ने अपनाया. उर्दू शायरी हमेशा शुक्र गुज़ार रहेगी जनाब 'अहमद नदीम कासमी' साहब की,जिन्होंने 'शकेब' की शायरी को उनके इंतकाल के छै साल बाद प्रकाशित करवा और उन्हें दुनिया तक पहुँचाया. नदीम साहब की शायरी में 'शकेब' की झलक साफ़ दिखाई देती है
आकर गिरा था कोई परिंदा लहू में तर
तस्वीर अपनी छोड़ गया है चटान पर
मलबूस खुशनुमा हैं मगर जिस्म खोखले
छिलके सजे हों जैसे फलों की दुकान पर
मलबूस: वस्त्र
हक़ बात आके रुक सी गयी थी कभी 'शकेब'
छाले पड़े हुए हैं अभी तक ज़बान पर
अफ़सोस आज के दौर में ऐसी शायरी कहीं पढने सुनने को नहीं मिलती. शकेब की शायरी गुलाब के फूलों की टहनी है जिसमें कोमलता है खुशबू है और कांटे हैं. बदायूं उत्तर प्रदेश से अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद शकेब आगे की पढाई के लिए रावलपिंडी चले गए और फिर नौकरी के सिलसिले में लाहौर. अपनी शादी के दस साल बाद किन्हीं अज्ञात कारणों से उन्होंने रेल की पटरियों पर अपना सर रख कर ख़ुदकुशी कर ली. एक अत्यंत प्रतिभाशाली शायर का ये अंत बहुत दुखद था.
न इतनी तेज़ चले सरफिरी हवा से कहो
शज़र पे एक ही पत्ता दिखाई देता है
बुरा न मानिए लोगों की ऐबजोई का
उन्हें तो दिन का भी साया दिखाई देता है
ऐबजोई: दोष ढूंढना
ये एक अब्र का टुकड़ा कहाँ कहाँ बरसे
तमाम दश्त ही प्यासा दिखाई देता है
खालिस याने बिना किसी मिलावट के शायरी पसंद करने वालों के लिए ये किताब किसी नियामत से कम नहीं. इसके हर पन्ने पर शायरी अपने पूरे शबाब पर फैली दिखाई देती है. मिसरे ठिठकने पर मजबूर करते हैं और शेर दांतों तले उँगलियाँ दबाने पर. इस किताब को पढने के बाद हुए असर को लफ़्ज़ों में बयाँ नहीं किया जा सकता इसके लिए आपको इसे पढना ही होगा. किनारे पर बैठ कर लहरें गिनने से समंदर की गहराई का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता.
मुरझा के काली झील में गिरते हुए भी देख
सूरज हूँ मेरा रंग मगर दिन ढले भी देख
आलम में जिसकी धूप थी उस शाहकार पर
दीमक ने जो लिखे कभी वो तब्सिरे भी देख
शाहकार: कृति, तब्सिरे: समीक्षाएं
बिछती थीं जिसकी राह में फूलों की चादरें
अब उसकी ख़ाक घास के पैरों तले भी देख
डायमंड बुक्स वालों का इस किताब के प्रकाशन के लिए और श्री सुरेश कुमार का संपादन के लिए शुक्रिया अदा करते हुए मुझे इस सफ़र को न चाहते हुए भी यहीं ख़तम करना होगा. आप अगर इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी 011-51611861-865 पर फोन करें या फिर उन्हें
sales@diamondpublication.com पर मेल करें. ‘शकेब’ की शायरी को आपतक पहुँचाने का लालच रोके नहीं रुक रहा सो चलते चलते उनके कुछ मुत्फ़रिक से शेर आप तक पहुंचा रहा हूँ.
आज भी शायद कोई फूलों का तोहफा भेज दे
तितलियाँ मंडरा रहीं हैं कांच के गुलदान पर
***
सोचो तो सिलवटों से भरी है तमाम रूह
देखो तो इक शिकन भी नहीं है लिबास में
***
जो मोतियों की तलब ने कभी उदास किया
तो हम भी राह से कंकर समेट लाये बहुत
***
दोस्ती का फ़रेब ही खाएं
आओ काग़ज़ की नाव तैरायें
***
जंगल जले तो उनको खबर तक न हो सकी
छाई घटा तो झूम उठे बस्तियों के लोग
***
ढूंढती हैं तिरी महकी हुई जुल्फों की बहार
चांदनी रात के ज़ीने से उतर कर यादें
इस बेजोड़ शायरी की दाद देने के लिए न तो हमारे पास शायर का फोन नंबर है और न ही मोबाइल नंबर और तो और उसका पता भी नहीं है इसलिए चलिए उसे दिल से याद करते हैं और दुआ करते हैं वो ज़िन्दगी के सारे झमेलों से दूर जहाँ है वहाँ सुकून से रहे. आमीन. मजरूह साहब का एक मकबूल शेर याद आ रहा :-
ज़माने ने मारे जवां कैसे कैसे
ज़मीं खा गयी आसमां कैसे कैसे

जनाब शकेब जलाली साहेब