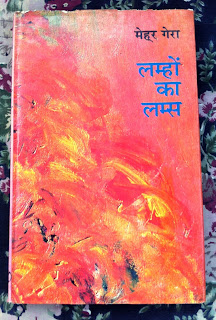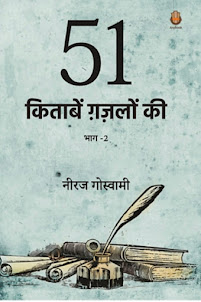लोग फिर भी घर बना लेते हैं भीगी रेत पर
जानते हैं बस्तियां कितनी समंदर ले गया
उस ने देखे थे कभी इक पेड़ पर पकते समर
साथ अपने एक दिन कितने ही पत्थर ले गया
समर: फल
रुत बदलने तक मुझे रहना पड़ेगा मुन्तजिर
क्या हुआ पत्ते अगर सारे दिसंबर ले गया
मुन्तजिर: इंतज़ार में
पुस्तक मेले में हिंदी भाषा की पुस्तकों के पंडाल में मैंने बहुत से हिंदी लेखकों को अपनी बात अंग्रेजी में रखते देख शर्म से गर्दन झुका ली। मैं अंग्रेजी का विरोधी नहीं लेकिन जो भाषा हमारी अपनी है उस से सौतेला व्यवहार करना मुझे पसंद नहीं आता।
वो बार बार बनाता है एक ही तस्वीर
हरेक बार फकत रंग ही बदलता है
गजाले -वक्त बहुत तेज़-रौ सही लेकिन
कहाँ पे जाय कि जंगल तमाम जलता है
गजाले-वक्त: समय का हिरन
अजीब बात है जाड़े के बाद फिर जाड़ा
मेरे मकान का मौसम कहाँ बदलता है
मैं हूँ बिखरा हुआ दीवार कहीं दर हूँ मैं
तू जो आ जाय मेरे दिल में तो इक घर हूँ मैं
कल मेरे साथ जो चलते हुए घबराता था
आज कहता है तिरे कद के बराबर हूँ मैं
इससे मैं बिछडू तो पल भर में फना हो जाऊं
मैं तो खुशबू हूँ इसी फूल के अंदर हूँ मैं
जितनी जानकारी मुझे मिली है उसके अनुसार गेरा साहब का जन्म एक मई 1933 को पंजाब में जालंधर के पास हुआ। उनकी दो किताबें शाया हुई हैं पहली 'पैकार' और दूसरी " लम्हों का लम्स" जिसके लिए सन 1992 में उन्हें आल इण्डिया मीर अकादमी लखनऊ की और से मीर एवार्ड मिला।
ये दायरे तेरी नश्वो-नुमा में हायल हैं
जरा तू सोच बदल कैद से निकल तो सही
नश्वो-नुमा:विकास, हायल: रूकावट
गवाँ न जान यूँही मंजिलों के चक्कर में
सफ़र का लुत्फ़ उठा ज़ाविया बदल तो सही
ज़ाविया "दृष्टिकोण
कहीं वजूद ही तेरा न इसमें खो जाए
बड़ा हजूम है इस शहर से निकल तो सही
तिरे वजूद की खुशबू का पैरहन पहना
तिरे ही लम्स को ओढ़ा तिरा बदन पहना
वजूद:अस्तित्व, लम्स:स्पर्श
वो शख्स भीग के ऐसे लगा मुझे जैसे
कँवल के फूल ने पानी बदन बदन पहना
तिरे बदन की जिया इस तरह लगे जैसे
इक आफताब को तूने किरन किरन पहना
जिया :रौशनी
रुत बदलते ही हर-इक सू मोजज़े होने लगे
पेड़ थे जितने भी सूखे सब हरे होने लगे
ये सफ़र में आ गया कैसा मुकामे-इंतेशार
लोग क्यूँ इक दुसरे से दूर अब होने लगे
मुकामे-इंतेशार:बिखराव का मुकाम
भूलकर सब कुछ समेटें क्यूँ न हम लम्हों का लम्स
ये भी क्या मिलते ही फिर शिकवे-गिले होने लगे