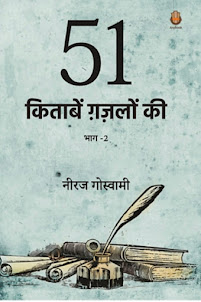आसमानों की बुलंदी में कहाँ आया ख्याल
इक नशेमन भी बना लूँ चार तिनके जोड़कर
बेयक़ीनी ने ये कैसा ख़ौफ़ मुझमें भर दिया
अब कहीं जाता नहीं मैं खुद को तनहा छोड़कर
कम से कम दस्तक ही देकर देख लेता एक बार
मुझमें दाख़िल क्यों हुआ वो शख़्स मुझको तोड़कर
ये बाकमाल लहज़ा , लफ़्ज़ों को बरतने का ये हुनर और कहन का ये दिलचस्प अंदाज़, शायरी के दीवाने बखूबी जानते हैं कि ये लखनऊ स्कूल की देन है जो जनाब 'मीर तकी मीर' साहब से शुरू हुई. इसी 'लखनऊ स्कूल' की गंगा जमुनी तहज़ीब की गौरव शाली परम्परा को उनके बाद सौदा ,नासिख़ ,मज़ाज़ ,जोश, आनंद नारायण मुल्ला ,वाली आसी, कृष्ण बिहारी नूर जैसे शायरों ने आगे बढ़ाया और अब उसी परम्परा को मुनव्वर राणा, भारत भूषण पंत और ख़ुशबीर सिंह 'शाद' के साथ युवा शायर अभिषेक शुक्ला और मनीष शुक्ला बहुत ख़ूबसूरती से आगे बढ़ा रहे हैं।
हमारे आज के मोतबर शायर हैं जनाब ' ख़ुशबीर सिंह 'शाद' "साहब जिनकी हाल ही में देवनागरी लिपि में एनीबुक द्वारा प्रकाशित किताब 'शहर के शोर से जुदा' की बात हम करेंगे।
ये भी मुमकिन है कि खुद ही बुझ गए हों चराग़
बेगुनाही किसलिए अपनी हवा साबित करे
तेरे सजदे भी रवा, तेरी इबादत भी क़ुबूल
शर्त ये है ख़ुद को तू पहले ख़ुदा साबित करे
अपने ख़द्दो- खाल की ख़ुद ही गवाही दूंगा मैं
क्यों मिरि पहचान कोई दूसरा साबित करे
लखनऊ स्कूल की गंगा जमुनी शायरी की तहज़ीब को 'ख़ुशबीर' साहब ने अपने उस्ताद 'वाली आसी' साहब की शागिर्दी में सीखा। जनाब 'वाली आसी' साहब के बारे में हम 'भारत भूषण पंत' साहब की किताब 'बेचेहरगी' की चर्चा के दौरान बता चुके हैं , उनके शागिर्दों में मुनव्वर राणा भी शामिल थे। मुशायरों के मंच पर अंधड़ की तरह चल रही शायरी के बीच 'शाद' साहब की शायरी सुबह के वक्त मंद मंद चलती पुरवाई की तरह महसूस होती है।
हो तो गए बहाल तअल्लुक़ सभी मगर
दिल में जो इक ख़लिश थी पुरानी, नहीं गयी
वो रात इक कनीज़ के सपनो की रात थी
उस रात ख़्वाब गाह में रानी नहीं गयी
लफ़्ज़ों को फिर गवाह बनाया गया है 'शाद'
अश्कों की इक दलील भी मानी नहीं गयी
4 सितम्बर 1954 को सीतापुर उत्तर प्रदेश में जन्में 'शाद' ने अपनी पढाई 'सिटी मोंटेसरी स्कूल' लखनऊ और 'क्राइस्ट चर्च कॉलेज' लखनऊ से की। उनके पिता चाहते थे कि वो उनकी आलमबाग ,जहाँ वो रहते थे, वाली प्रिंटिंग प्रेस को संभालें लेकिन उनका भाग्य उन्हें कोई दूसरी ही दिशा में ले गया। बचपन से ही उन्हें कविताओं से प्रेम था तभी उन्होंने हिंदी के लगभग सभी कवियों की रचनाओं को पढ़ डाला। शायरी की तरफ झुकाव हुआ तो उन्होंने 'सुल्तान खान 'साहब से बाकायदा उर्दू की तालीम ली। धीरे धीरे शेर कहने लगे। अमीनाबाद में उन दिनों साहित्य प्रेमियों की महफ़िल लगा करती थी ,वहीँ 'शाद' साहब ने जनाब 'वाली आसी' साहब को अपने शेर सुनाये। उनके शेरों और कहन से प्रभावित हो कर 'वाली आसी ' साहब ने उन्हें अपनी शागिर्दी में रख लिया।
मैं आज़िज़ आ चुका हूँ अपनी गैरत की नसीहत से
ये कहती है कि जो करना वो मुझसे पूछ कर करना
मिरि मिटटी तुझे चूमूँ कि आँखों से लगाऊं मैं
तिरा ही हौसला है एक कोंपल को शजर करना
बहुत समझाया मैंने हाशियों की क्या जरुरत है
मगर वो चाहता था दास्ताँ को मुख़्तसर करना
मुझे मालूम है मेरे बिना वो रह नहीं सकता
कहीं भटका हुआ मिल जाय तो मुझको ख़बर करना
अपनी पहली किताब 'जाने कब ये मौसम बदले' जो 1992 में शाया हुई थी के बाद उन्होंने मुड़ कर नहीं देखा और लगातार शेर कहते रहे नतीज़ा ये हुआ कि अब तक उनके नौ मज़्मुए शाया हो चुके हैं जिन में से तीन तो उर्दू अकेडमी उत्तर प्रदेश द्वारा पुरुस्कृत हो चुके हैं। उनकी शेष किताबों के उन्वान इस तरह हैं "गीली मिटटी (1998) ", 'ज़रा ये धूप ढल जाय (2005)", "बेख्वाबियाँ (2007) ","जहाँ तक ज़िन्दगी है (2009)","बिखरने से जरा पहले (2011)", "लहू की धूप (2012)", "बात अंदर के मौसम की (2014)" इसके अलावा उनकी एक किताब "चलो कुछ रंग ही बिखरे (2000)" को पाकिस्तान के जाने माने प्रकाशक 'वेलकम बुक पोर्ट' ने प्रकाशित किया है।
मिरि दरियादिली उतरे हुए दरिया की सूरत है
ये हसरत ही रही दिल में किसी के काम आऊं मैं
ये कैसी कश्मकश ठहरी हमारे दरमियाँ दुनिया
न मुझको रास आये तू, न तुझको रास आऊं मैं
किसी दिन लुत्फ़ लूँ मैं भी तिरे हैरान होने का
किसी दिन बिन बताये ही तिरी महफ़िल में आऊं मैं
बस इक ज़िद ही तो हाइल है हमारे दरमियाँ वरना
अगर पहले मनाये वो तो शायद मान जाऊं मैं
बहुत ही कम शायर हैं जो मुशायरों में सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए अपनी शायरी से समझौता नहीं करते और ख़ास तौर पर ऐसे शायर जिनकी रोज़ी रोटी ही इस से चलती हो वो तो बहुत ही संभल कर मंच पर अपनी रचनाएँ सुनाते हैं। जनाब ख़ुशबीर सिंह साहब अपवाद हैं उन्होंने कभी शायरी के मेयार से समझौता नहीं किया,तालियां बटोरने के लिए हलकी शायरी नहीं की क्यूंकि इसकी उन्हें कभी जरुरत ही महसूस नहीं हुई। उनकी शायरी इतनी खूबसूरत और दिलकश होती है कि श्रोता बार बार तालियां बजाते हुए और और सुनने की फरमाइश करते हैं। हक़ीक़त ये है कि आज भी लोग अच्छी शायरी के दीवाने हैं लेकिन क्यूंकि अच्छा कहने वाले बहुत कम हैं इसलिए वो लफ़्फ़ाज़ी सुनने के लिए मज़बूर हैं।
तिरि कुर्बत भी मुझको रास हो ऐसा नहीं फिर भी
अकेलेपन से डरता हूँ मुझे तनहा न छोड़ा कर
कुर्बत =समीपता
नहीं ! अच्छा नहीं लगता मुझे यूँ मुन्तशिर होना
मेरी लहरों में अपनी याद के पत्थर न फेंका कर
मुन्तशिर = बिखर हुआ
तुझे अलफ़ाज़ के पैकर ही में हर बात दिखती है
कभी खामोशियों को भी सुना कर और समझा कर
'शाद' साहब के चाहने वाले पूरी दुनिया में फैले हुए हैं उन्हें 'अमेरिका , यूनाइटेड अरब एमिराईट , पाकिस्तान ,दोहा, ओमान, बेहरीन,दुबई, अबू धाबी और सिंगापुर आदि में अपनी शायरी सुनाने का मौका मिल चुका है. उनके इंटरव्यू और शायरी भारत और पाकिस्तान के प्रमुख अखबारों और पत्रिकाओं में लगातार प्रकाशित होती रहती है। दोनों मुल्कों के टी वी पर भी उन्हें चाव से देखा सुना जाता है। दूरदर्शन पंजाबी ने तो उन पर एक वृत्त चित्र का निर्माण कर उसे प्रदर्शित भी किया है। जम्मू यूनिवर्सिटी ने एक विद्यार्थी को उनके साहित्य पर शोध के लिए 'एम् फिल' की डिग्री प्रदान की है।
किसी के बस में कहाँ था कि आग से खेले
मिरे क़रीब कोई इक मिरे सिवा न गया
मैं एक फूल की वुसअत में रह के जी लेता
मगर हवा ने पुकारा तो फिर रहा न गया
वुसअत =फैलाव
था मेरे गिर्द बहुत शोर मेरे होने का
मैं जब तलक तेरी खामोशियों में आ न गया
'शाद' साहब को उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए जो पुरूस्कार मिले हैं अगर उनकी गिनती की जाय तो ये पोस्ट छोटी पड़ जाएगी सारे तो नहीं लेकिन कुछ चुनिंदा पुरूस्कार इस तरह हैं नार्थ अमेरिका की अंजुमन-ऐ-तरक्की द्वारा पोएट ऑफ दी ईयर अवॉर्ड ,अमेरिकन इस्लामिक कांग्रेस अवार्ड ,हसरत मोहानी अवॉर्ड पकिस्तान ,जश्ने अदब ऐज़ाज़ अवॉर्ड श्री गोपी चंद नारंग द्वारा,लोक लिखारी अवॉर्ड पंजाब ,और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया 'यश भारती' अवॉर्ड।
उसी वुसअत से जिसके पार जाना गैर मुमकिन था
मैं आगे बढ़ गया हद्दे-नज़र से मश्विरा करके
वुसअत = फैलाव
मसाइल ज़िन्दगी के खुद ब खुद आसान हो जाएँ
कभी देखो किसी आशुफ्ता सर से मश्विरा करके
मसाइल =समस्या , आशुफ्ता सर =पागल, सिरफिरा
जवाँ बच्चों की अपनी ज़िन्दगी है उनसे क्या शिकवा
जुदा होते हैं क्या पत्ते शजर से मश्विरा करके
"शहर के शोर से जुदा" में 'शाद' साहब की लगभग 90 ग़ज़लें संग्रहित हैं , एनीबुक के पराग अग्रवाल ने गागर में सागर भरने का प्रयास किया है जिसमें वो बहुत हद तक क़ामयाब भी हुए हैं. 'शाद' साहब के कलाम को किसी भी एक किताब में समेटा ही नहीं जा सकता ,इस किताब में पराग साहब ने ग़ज़लों ने बाद उनकी कुछ और ग़ज़लों के फुटकर शेर भी प्रकाशित किये हैं जिनमें से अधिकतर उनकी पहचान बन चुके हैं। किताब में मुश्किल उर्दू लफ़्ज़ों का हिंदी में अर्थ न देना आम पाठक को अखर सकता है, हो सकता है कि अगले संस्करण में इस कमी को प्रकाशक द्वारा पूरा लिया जाय।
इस किताब की प्राप्ति के लिए आप पराग को उनके मोबाइल 9971698930 पर संपर्क करें और 'शाद'साहब को, जो अब जालंधर रहते हैं, उनके मोबाइल 09872011882 पर संपर्क कर दिल से बधाई दें। वैसे ये किताब अमेज़न पर भी उपलब्ध है
आईये आपको चलते चलते ख़ुशबीर साहब के कुछ ऐसे शेर पढ़वाता हूँ जो उनकी पहचान बन चुके हैं :-
मिरी मर्ज़ी के मुझको रंग देदे
तो फिर तस्वीर मेरी ज़िम्मेवारी
***
कैसी बेरंगियों से गुज़रा हूँ
ज़िन्दगी तुझमें रंग भरते हुए
***
थकन जो जिस्म की होती उतार भी लेते
तमाम रूह थका दी है इस सफर ने तो
***
तुमने इक बात कही दिल पे क़यामत टूटी
इक शरर कम तो नहीं आग लगाने के लिए
***
मुठ्ठी में किर्चियों को ज़रा देर भींच लो
फिर उसके बाद पूछना कैसे जिया हूँ मैं
***
ये तेरा ताज नहीं है हमारी पगड़ी है
ये सर के साथ ही उतरेगी सर का हिस्सा है