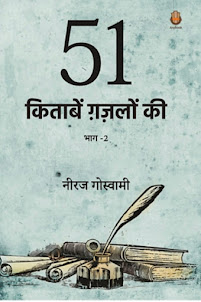चलिए "किताबों की दुनिया" श्रृंखला की आज की कड़ी शुरू करने से पहले आपको कुछ फुटकर शेर पढ़वाते हैं जो इस पोस्ट के मिज़ाज़ को बनाए रखने में सहायक होंगें। आपने अगर पहले से ही ये शेर पढ़े हैं तो आपको इस बाकमाल शायर के बारे में बहुत कुछ बताने की जरुरत नहीं पड़ेगी और नहीं पढे तो हम तो हैं ही बताने को
छतरी लगा के घर से निकलने लगे हैं हम
अब कितने एहतियात से चलने लगे हैं हम
हो जाते हैं उदास कि जब दो-पहर के बाद
सूरज पुकारता है कि ढलने लगे हैं हम
****
न आँख में कोई आंसू न हाथ में कोई फूल
किसी को ऐसे सफर पर रवाना करते हैं ?
****
हमें अंजाम भी मालूम है लेकिन न जाने क्यों
चरागों को हवाओं से बचाना चाहते हैं हम
****
जरा सी धूप चढ़ेगी तो सर उठाएगी
सहर हुई है अभी आँख मल रही है हवा
****
शरारतों का वही सिलसिला है चारों तरफ
कहाँ चराग जलाएं हवा है चारों तरफ
आपको बता देता हूँ कि ये लाजवाब शेर उस्ताद शायर जनाब "
वाली आसी " साहब के हैं जिनकी किताबों की दुकान "
मकतब-ऐ-दीनो अदब " जहाँ व्यापार कम और अदब की खिदमत ज्यादा की जाती थी ,पर लखनऊ के तमाम छोटे-बड़े शायरों और तालिब-ऐ- इल्म का जमावड़ा हुआ करता था। उर्दू शायरी के दीवाने उनसे गुफ्तगू करने और शायरी के नए अंदाज़ सीखने , इस्लाह लेने के लिए जमा होते थे। उनके बहुत से मुस्लिम और गैर मुस्लिम शागिर्द हुए जिन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा और शायरी में आला मुकाम हासिल करने के साथ साथ उनका और अपना नाम भी रौशन किया। उन्हीं के एक गैर मुस्लिम शागिर्द जिनके उस्ताद भाई "मुनव्वर राणा" हैं की किताब हम आज आपके लिए लाये हैं।
चाहतों के ख्वाब की ताबीर थी बिलकुल अलग
और जीना पड़ रही है ज़िन्दगी बिलकुल अलग
और कुछ महरूमियाँ भी ज़िन्दगी के साथ हैं
हर कमी से है मगर तेरी कमी बिलकुल अलग
महरुमियाँ = कमियाँ
आईने में मुस्कुराता मेरा ही चेहरा मगर
आईने से झाँकती बेचेहरगी बिलकुल अलग
जनाब "
भारत भूषण पंत " साहब की ग़ज़लों की किताब "
बेचेहरगी " ,जिसका जिक्र हम करने जा रहे हैं ,का एक एक शेर इस बात की गवाही देता है कि एक शागिर्द के लिए आला
दर्ज़े के उस्ताद की एहमियत क्या होती है और अच्छा शेर कहना किस कदर सलीके का काम है। उनकी हर ग़ज़ल गहरी सोच का परिणाम है। एक ऐसी शायरी जिसमें ज़िन्दगी अपने सभी रंगों के साथ नज़र आती है। यूँ कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि अगर आपको ज़िन्दगी के रंग शायरी के संग देखने हों तो भारत भूषण पंत साहब को पढ़ें ।
दिल का बोझ यूँ हल्का तो हो जाता है
लेकिन
रोने से अश्कों की भी अरजानी होती है
अरजानी = नुक्सान , बेकार जाना
रंज उठाने की तो आदत पड़ ही जाती है
मुश्किल तब होती है जब आसानी होती है
हम भी ऐसे हो जायेंगे किसने सोचा था
अपनी सूरत देख के अब हैरानी होती है
फ्रेंच कट दाढ़ी भारत भूषण जी के चेहरे पर फबती तो है लेकिन अमिताभ बच्चन की तरह उनकी पहचान नहीं बनती क्यों कि उनकी असली पहचान तो उनकी शायरी के हवाले से है। बेहद संजीदा किस्म के शायर पंत साहब अपने बारे में ज्यादा नहीं बोलते लेकिन उनकी शायरी सुनने वालों के सर चढ़ कर बोलती है। आज के मंचीय शायरों को जो मुशायरों में सामईन से अपने हर शेर पर दाद की भीख मांगते हैं पंत साहब से ये बात सीखनी चाहिए की अगर शेर में दम होगा तो दाद-खुद-ब खुद सुनने वालों के मुंह से निकलेगी।
वक्त से पहले सूरज भी कब निकला है
खुद को सारी रात जला कर क्या होगा
तब तक तो ये बस्ती ही जल जाएगी
अपने घर की आग बुझा कर क्या होगा
इन कपड़ों में यादों जैसी सीलन है
इन कपड़ों को धूप दिखा कर क्या होगा
यूँ तो कभी ये ज़ख्म नहीं भर पाएंगे
दीवारों से सर टकरा कर क्या होगा
3 जून 1958 को जन्मे भारत भूषण जी का स्थायी निवास लखनऊ ही रहा है यहीं से इन्होने शिक्षा प्राप्त की और यहीं के एक कोऑपरटिव बैंक में काम किया। व्यक्तिगत कारणों से सन 2011 वी आर एस लेने के बाद अब वो पूर्ण रूप से लेखन को समर्पित हैं। अपने आसपास और भीतर की दुनिया को देखने समझने का उनका अपना तरीका है, वो जो महसूस करते हैं उसी को बहुत ईमानदारी के साथ अपनी शायरी में ढाल देते हैं। पंत साहब की शायरी में मन की बेचैनी तो है लेकिन साथ ही तेज धूप में किसी घने बरगद के तले मिलने वाले सुकून का एहसास भी है।
यही तन्हाइयाँ हैं जो मुझे तुझसे मिलाती हैं
इन्हीं खामोशियों से तेरा चर्चा रोज़ होता है
ये इक एहसास है ऐसा किसी से कह नहीं सकता
तेरी मौजूदगी का घर में धोका रोज़ होता है
ये मंज़र देख कर हैरान रह जाती हैं मौजें भी
यहाँ साहिल पे इक टूटा घरौंदा रोज़ होता है
मैं इक किरदार की सूरत कई परतों में जीता हूँ
मेरी बेचेहरगी का एक चेहरा रोज़ होता है
उर्दू और हिंदी दोनों लिपि में एक साथ छपी "
बेचेहरगी" पंत साहब की तीसरी ग़ज़लों की किताब है जो सन 2010 में प्रकाशित हुई थी , इसमें उनकी 70 लाजवाब ग़ज़लें संगृहीत हैं. इससे पूर्व उन्ही पहली किताब "तन्हाइयाँ कहती हैं " सुमन प्रकाशन आलमबाग से सन 2005 में और "यूँ ही चुपचाप गुज़र जा " सन 1995 में प्रकाशित हो कर मकबूल हो चुकी है। उनकी आज़ाद नज़्मों की किताब सन 1988 में "कोशिश" शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। उनके उस्ताद भाई मुनव्वर लिखते हैं कि " भारत भूषण ने अपनी शायरी को हमेशा सिसकियों की छत्रछाया में रखा है, किसी भी लफ्ज़ को चीख नहीं बनने दिया। अपनी हर ग़ज़ल में वो अपने दुखों से खेलते दिखाई देते हैं "
हर घडी तेरा तसव्वुर, हर नफ़स तेरा ख्याल
इस तरह तो और भी तेरी कमी बढ़ जायेगी
तसव्वुर : कल्पना , नफ़स : सांस
उसने सूरज के मुकाबिल रख दिए अपने चिराग
वो ये समझा इस तरह कुछ रौशनी बढ़ जायेगी
तू हमेशा मांगता रहता है क्यूँ ग़म से निजात
ग़म नहीं होंगे तो क्या तेरी ख़ुशी बढ़ जायेगी ?
क्या पता था रात भर यूँ जागना पड़ जायेगा
इक दिया बुझते ही इतनी तीरगी बढ़ जायेगी
तीरगी : अँधेरा
शमीम आरज़ू साहब ने लखनऊ सोसाइटी की साईट पर लिखा है कि" भारत भूषण पंत की शाइरी अहसास की शाइरी है. वह मुशायरे नहीं लूटती लेकिन किसी शिकस्तादिल शख्स की ग़मगुसारी और चारासाज़ी बखूबी करती है. ये वो सिफत है जो हर किसी के हिस्से में नहीं आती है. क्योंकि इसका अहतराम करने के लिए खुलूस और हिस्सियत के जिन नाज़ुक दिल जज्बात की ज़रूरत होती है वो अक्सर मुशायरों की तालियों से खौफ खाते हैं. पंत साहब को अदबी खेमों का हिस्सा बनना भी नहीं आता. लेकिन गेसू-ए-गज़ल को संवारना उन्हे खूब आता है"
कुछ तो घरवालों ने हमको कर दिया माज़ूर सा
और कुछ हम फितरतन उक्ता गए घरबार से
माज़ूर -मज़बूर
तेरे सपनों की वो दुनिया क्या हुई, उसको भी देख
हो चुकी हैं नम बहुत ,आँखें उठा अखबार से
सबसे अच्छा तो यही 'ग़ालिब' तेरा जामे-सिफाल
टूट भी जाये तो फिर ले आईये बाजार से
जामे-सिफाल -मिटटी का प्याला
इस किताब का जिक्र लखनऊ के शायर मेरे अज़ीज़ अखिलेश तिवारी जी के बिना पूरा नहीं होगा क्यूंकि उन्हीं की बदौलत ये किताब मुझे इस शर्त पर पढ़ने को मिली कि मैं इसे पढ़ते ही उन्हें वापस लौटा दूंगा। अखिलेश का ये उपकार मैं कैसे चुकाऊं ये मेरे लिए अब शोध का विषय बन गया है। जिनके पास अखिलेश जैसे मददगार नहीं हैं उनको इस किताब प्राप्ति के लिए यूनिवर्सल बुक सेलर्स , हज़रतगंज , गौमती नगर लखनऊ को लिखना पड़ेगा या फिर भारत भूषण जी को उनके मोबाईल न 9415784911 पर संपर्क करना पड़ेगा। यकीन मानें आपके द्वारा इस अनमोल किताब की प्राप्ति के लिए किया गया कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जायेगा।
भरे घर में अकेला मैं नहीं था
दरो -दीवार थे, तन्हाइयाँ थीं
लड़कपन के मसायल भी अजब थे
पतंगे थीं, उलझती डोरियाँ थीं
मसायल =विषय
बहुत उकता गया था दिल हमारा
कई दिन से मुसलसल छुट्टियाँ थीं
हमारी दास्ताँ में क्या नहीं था
हवा थी, बारिशें थीं, बिजलियाँ थीं
शायरी करने वालों और सीखने वालों के लिए इस किताब में बहुत कुछ है जैसे शेर में लफ्ज़ किस तरह कितने और कहाँ बरतने चाहिए। सीधी सरल बोलचाल की भाषा में अपनी बात शायराना ढंग से रखने का फन ये किताब वर्क दर वर्क सिखाती है। आखिर में फिर से मुनव्वर राणा साहब की इस बात को आपतक पहुंचा कर आपसे से विदा लेते हैं " एक नौजवान जिसकी मादरी ज़बान हिंदी हो जिसने उर्दू मेहनत करके सीखी हो जो एक छोटे से बैंक में एक छोटी सी पतवार के सहारे अपनी ज़िन्दगी की कश्ती को मसायल और उलझनों के दरया में सलीके से चला रहा हो , मुशायरों से कोई दिलचस्पी न रखता हो , अपने आपको अकेलेपन की ज़ंज़ीर में जकड़े हुए हो, जो चेहरे पर हमेशा एक बोझिल सी मुस्कराहट चिपकाये हुए शहर की सड़कों पर किसी फ़साद में जली हुई किताब के वरक की तरह टूटता बिखरता और उड़ता चला जा रहा हो यकीनन वो कोई ऐसा मुसव्विर (चित्रकार) होगा जो कलम से कागज पर शायरी नहीं मुसव्वरी कर रहा होगा, आइए हम ऐसे शायर का सूफी मंश इंसान का इस्तेकबाल करें। यही इस शायर का ईनाम भी होगा और मेहनताना भी "
मुसव्विर अपने फन से खुद भी अक्सर ऊब जाते हैं
अधूरे ही बना कर कितने मंज़र छोड़ देते हैं
बहुत से ज़ख्म हैं ऐसे जो देखे भी नहीं जाते
जहाँ घबरा के चारागर भी नश्तर छोड़ देते हैं
कभी जब जमने लगती हैं हमारी सोच की झीलें
तो हम ठहरे हुए पानी में पत्थर छोड़ देते हैं
पोस्ट कुछ लम्बी जरूर हो गयी है लेकिन जब शायर बेहतरीन हो तो ऐसी बातें नज़र अंदाज़ कर देनी चाहिए। अगली किताब की तलाश में निकलने से पहले एक आखरी शेर और पढ़ते चलें :
सच कहूं तो मौजों से डर मुझे भी लगता है
क्या करूँ किनारों पर नाव चल नहीं सकती